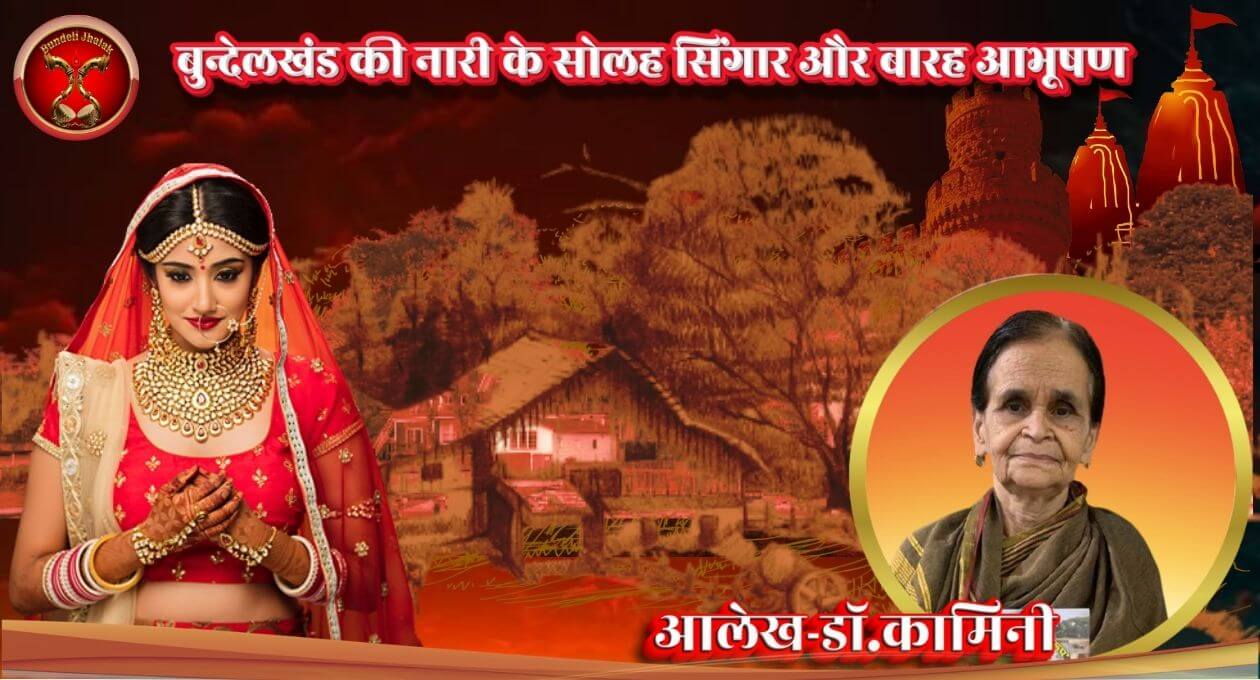सोलह सिंगार और बारह आभूषणों Solah Sringar Aur Barah Abhushan की परिपाटी भी स्थान विशेष और काल-विशेष में परिवर्तित होती रही है। उबटन से लेकर शशिफूल तक बारह आभूषणों ने भी कई रूप धारण किये हैं। Solah Sringar Aur Barah Abhushan नारी की श्रृंगार प्रियता का गिना जाने योग्य स्वरूप है।

मानव-समाज की महत्त्वपूर्ण संस्था परिवार है। परिवार के मूल में स्त्री और पुरुष दोनों हैं। स्त्री परिवार को सुखकर बनाती है। इसीसे उसे जीवन रस का अक्षय कोश माना गया है। स्त्रियों की श्रृंगार-साधना लम्बा मार्ग तय करके वर्तमान तक आई है। श्रृंगार प्रियता स्त्री की आदिम ललक है।
किसी भी कालखंड में स्त्री श्रृंगार से विरक्त नहीं हुई। आभूषण, स्त्री की कमजोरी है। प्रकृति ने शरीर और हृदय से नारी को कोमल बनाया है। यही कोमलता उसे पुरुष के समीप लाती श्रृंगार के प्रति आकर्षण पैदा करती है और सजने संवरने की लालसा को निरंतर बनाये रखती है।
सोलह सिंगार के अंतर्गत सर्वप्रथम उबटन आता है। शरीर को काँतिवान और सुगंधित बनाने के लिए उबटन का उपयोग किया जाता रहा है। इसके बाद स्नान की बारी आती है। तीसरा सिंगार सुंदर वस्त्र धारण करना है, जो इस क्षेत्र में लँहगा, लुंगरा, बांड़, कस्बी, अँगिया और चोली से बढ़ते-बढ़ते साया, साड़ी और ब्लाउज तक आ पहुँचे है। चौथा श्रृंगार बाल सँवारना है। कंघी का आँचलिक स्वरूप ककई, ककवा है।
इस अंचल में दांई और बांई कनपटी के बालों को तीन बल में गुहकर ‘फिटियाँ’ बाँधी जाती थीं और इन फिटियों के दोनो सिरे पीछे जाकर चोटी में समाहित हो जाते थे। चोटी के बालों को भी तिवल करके गुह दिया जाता था। बाल संवारने के बाद फूलों के गजरे जूड़े से बाँधना आज भी यथावत है किंतु अब फिटियाँ गुहना लोक-जीवन से विदा हो चुका है।
पाँचवाँ श्रृंगार नेत्रों में काजल आँजना है। काजल आँजने की विधियाँ प्रस्तर प्रतिमाओं से होती हुई चित्रों तक आई और काजल के विभिन्न स्वरूप आज भी प्रचलित हैं। सिंदूर से माँग भरना और पैरों में महावर लगाना छठवें और सातवें श्रृंगार हैं। भाल पर तिलक, चिबुक पर तिल मेंहदी और सुगंध आठवें से लेकर ग्यारहवें क्रम तक के श्रृंगार हैं ।
सुगंध लेपन के द्रव्य देशकाल के अनुकूल चंदन हैं। बारहवें श्रृंगार के अंतर्गत आभूषण धारण करना आता है । तेरहवां श्रृंगार फूलों की माला पहिनना है। मिस्सी लगाना, पान खाना और होठों को लाल करना अंतिम तीन श्रृंगार क्रियायें हैं। इनमें से मिस्सी लगाना ठेठ गांव देहात से भी उठ गया है फिटकरी, हर्रा, कौसीस और मांजूफल के बराबर भागों को मिलाकर मिस्सी बनाई जाती थी।
बारह आभूषणों के अंतर्गत नूपुर, चूडी, हार, कंकन, अंग चिरियों, टीका, शीशफूल, किंकिणी और कंठश्री आती है। इन बारह आभूषणों ने बुंदेलखंड में बहुत रूप बदले है। नूपुर का आंचलिक स्वरूप हुआ बिछिया तक आया और आज विछिया सिकुड़कर बहुत छोटा आभूषण का नाम मीना हो गया। तीस-चालीस साल पहले बिरमिनी के संग अंगूठे में जोडुआ पहिने जाते थे। जोडुआ चाँदी की साँकल के द्वारा ‘पैती’ से जुडा रहता था।
चूड़ियाँ सामान्य रूप से काँच की ही पहनी जाती रही हैं। साउनी मे लाख की चूड़ियाँ भेजने का चलन था। विवाह के समय काँच के काले कचैहरा पहिने जाते थे , हार गले का आभूषण है। चाँदी के सिक्के को रेशमी धागे मे गुह कर पहिनने की परिपाटी से बढ़ते-बढ़ते आज हार का स्वरूप सोने के विभिन्न कटावों तक जा पहुँचा है। हमेल, खंगौरिया, लल्लरी, तिधानौं, गलबंद ठसी, साद्दानी, चंपाकली, चीलपट्टी, मटरमाला, मोहनमाला, नगमाला, लौकिट जंजीर के रूप में विस्तार हुआ है।
कंकन दोनों कलाइयों में पहना जाने वाला आभूषण है। जो चूरा, पटेला, चुरियाँ, ककना, ककनियाँ, गेंदगजरा, गुर्जें, दस्तबंद और गजरियों का मार्ग पार करता हुआ कंगन सैट और चूड़ी सेट तथा बेल चूडी में समाहित है। हाथ की उँगलियों में पहनी जाने वाली अंगूठी चाँदी और सोने की बनती रही हैं। पुरुष छला पहिनते थे। कंधा और कोहनी के मध्य भुजा पर पहना जाने वाला आभूषण बाजूबंद है। टड़ियाँ और तोरबंदी इसके परिवर्तित रूप हैं।
नाक और कान के आभूषण बाली बनाई जाती है। बेसर, पुंगरिया, लोंग और बारी में नाक का यह आभूषण संकचित और विस्तृत हुआ है। नथ को गूंज साधे रहती है। लोंग में नथुने के अंदर से पोला लगा दिया जाता है। कर्णफूल का प्रारम्भ चांदी की बारियों से हुआ होगा जो तरकियाँ, उतरंगा, झुमका, कन्नफूल, ऐरन, झुमका, टॉप्स, फूलमाला, झाला, लाला और बालों तक जा पहँचा है। तरकिया। कर्णफूल में साँकलें डालने का भी रिवाज था और माथे को घेरने वाला भी कर्णफूल से जुड़ी रहती थीं।
नवाँ आभूषण बैंदी है। शीशफूल, कि कंठश्री क्रमशः दसवें, ग्यारहवें और बारहवें आभूषण हैं। माथ का बैंदी, शीशफूल, झूमर और टीका से सम्मिलित हैं।
किंकणी की बनावट करधौनी और पेटी तक विकसित हुई है। झालरदार हॉफ करधनी भी चलन में है। पैरों का आभूषण ‘बोरीला’ विभिन्न आकार-प्रकार ग्रहण करता रहा है। लल्तपुरी पैजना की झलक, झाँसी की गूजरीं और दतिया के झिंझरया पैजना अपने समय के समर्थ आकर्षण रहे हैं। पंचमहल के चुल्ला, कड़ियाँ और तोड़ा आज भी ग्वालियर जनपद में अपना अस्तित्व बनाये हुए हैं। अनोखा, लच्छा, रूलें, पायजेब, छागल, पट्टे, पायल और तोड़ियाँ तक की यात्रा-कथा पैजनियाँ के अस्तित्व की यात्रा कथा है।
काले रंग की छड़याऊ बांड, अगउआ की तोई, गुलाबी चोली और शर्बती लँगरा, खंगौरिया, साँकरदार तरकियाँ, चूरा, पटेला, चुरियाँ, दौरी, पैजना, विरमिनी के साथ खिलखिल जाते थे। बुंदेलखंड में लोकजीवन की यह सामान्य वेश-भूषा अब क्रमशः तिरोहित होती जा रही है। आभूषण चलन से उठ गये। आने वाली पीढ़ी इन आभूषणों के नाम नहीं जानेगी।
सोलह सिंगार और बारह आभूषणों ने आदिम युग से लेकर वर्तमान तक विभिन्न आकार प्रकार धारण किये हैं। अनेक रुचियों में ढले और आकर्षण का अनुपमेय आश्रय रहे। जिस तरह परिवार के लिए नारी का सहयोग आवश्यक है, उसी तरह नारी की आदिम ललक को तुष्टि प्रदान करने के लिए सोलह सिंगार और बारह आभूषण सनातन हैं। बुंदेलखंड की नारी की शोभा सोलह सिंगार और बारह आभूषणों से है।