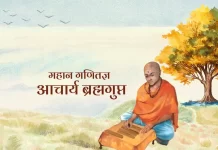चित्रण की प्रवृत्ति मनुष्य में तब से है जब वह जंगलों मे रहता था। रास्ता ढूँढने और उन्हे याद रखने के लिए जो चिन्ह बनाता था वह चित्रकला ही थी। Bhartiya Sanskriti Me Chitrakala लोक जीवन का एक अंग है । अपना सांस्कृतिक विकास करने के लिए संस्कृति के जिन अंगों से शुरूआत की उनमें चित्रकला भी एक थी। संसार भर में आदिम मनुष्य के अंकित चित्र मिलते हैं।
Painting in Indian Culture
ये विषय, शैली तथा सामग्री की दृष्टि से उस समय के मानव जीवन के प्रतीक हैं। इनके विषय मुख्यतः जानवर, उनका आखेट करते हुए मनुष्य, आपस में युद्ध करते हुए मनुष्य एवं पूजनीय आकृतियां हैं। ये रेखाचित्र प्रायः तत्कालीन मानव का निवास स्थल बनी प्राकृतिक कन्दराओं जिन्हें लोकभाषा में आज भी दरी कहा जाता है
दरी की दीवारों पर लाल गेरू या धाऊ पत्थर (हेमेटाइट) से बनाए गए हैं और लोकभाषा में उन्हीं के लिए रकत की पुतरियां शब्द प्रचलित है। इन स्थलों में भोपाल के समीप भीमबैठका, महादेव पहाड़ी के पचमढ़ी नामक स्थान के इर्द-गिर्द, रायगढ़ के समीप सिंघनपुर और काबरा पहाड़ के चित्र, मिर्जापुर क्षेत्र में लिखुनिया दरी, कोहबर दरी, मेहरिया दरी आदि मुख्य हैं।
प्रागैतिहासिक काल में ही आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिन्धु घाटी की सभ्यता के अन्तर्गत हमें विविध चित्रांकनों का निदर्शन होता है। सिन्धु सभ्यता में रंगे भाण्डों (बर्तनों ) और ठीकरों पर जो चित्रकारी हुई है, वह प्रायः पांच हजार वर्ष पहले के पूर्वजों के चित्र प्रेम की साख भरती है। इन भाण्डों और ठीकरों पर अनेक प्रकार की ज्यामितिक आकृतियां मिलती हैं, जो मुख्यतः काले और फीरोजी रंगों से बनी हैं।
हड़प्पा सभ्यता में उपलब्ध लगभग 1200 से अधिक घीया पत्थर की बनाई हुई मुहरें कला और लेखों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अधिकांश पर एक श्रृग पशु अंकित है, जिसकी पहचान ऋग्वेद के श्रृगवृष से की जा सकती है। अन्य पशुओं में महावृषभ, छोटे सींगों वाला नटुआ बैल, महिष, गैंडा, व्याघ्र, हाथी, खरगोश, हिरन, गरुड़, मगरमच्छ आदि हैं।
इनमें अंकित आकृतियों में एक श्रृग मुद्राओं पर स्तंभ भी प्रमुख हैं। स्तंभ के ऊपर कटोरा या वीरपात्र और उसके ऊपर वेदिका की खुली वेष्टनी या अण्डाकृति गूमठ- इन सबकी सम्मिलित कल्पना किसी देवता के ध्वजचिन्ह के रूप में की गई होगी। ऐतिहासिक युग के स्तंभों में सबसे ऊपर का भाग धर्मचक्र या सिंह, हाथी जैसे पशुओं से अलंकृत है।
हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं में वह स्थान वेदिकामय भाग का है, संभवतः इन स्तंभों पर भी वह भाग परवर्ती युगों की भांति वह देवसदन या विश्वदेवों का स्थान माना जाता था। स्तंभ के कई भागों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए ज्ञात होता है कि उसका सर्वप्रथम रूप सिन्धुघाटी की मुद्राओं पर है। स्तंभ पूजा की धार्मिक प्रथा का संबन्ध इन्द्र, प्रजापति एवं अन्य कई देवों से था ।
उत्तर वैदिक वाङमय में हम ऐसे शब्दों को पाने लगते हैं, जो पीछे चलकर चित्र के प्रसंग में प्रयुक्त हुए हैं। इनमें से एक शब्द छायातप है जो जगत के द्वन्द्व को परिलक्षित कराने में प्रयुक्त हुआ है। जातकों में जिस समाज का वर्णन है उसे हम चित्रकला में पूर्ण रूप से व्याप्त पाते हैं। जातकों में शिक्षा के अट्ठारह विषयों का उल्लेख है, जिनमें चित्रकला भी एक थी।
बुद्ध के समय चित्र इतने मोहक बनते थे कि बुद्ध ने भिक्षुओं को चित्र देखने की मनाही कर दी थी। तीसरी चौथी शताब्दी ई.पू. के बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक तथा थेरी गाथा में चित्रों का उल्लेख है।
वात्स्यायन के कामसूत्र में चित्र के छः अंग माने गए हैं, जो निम्ल श्लोक में वर्णित हैं-
रूपभेदाः प्रमाणानि भावलावण्ययोजनम।
सदृश्यं वर्णिकाभंगं इति चित्र षडंगकम
मानसोल्लास, कुमार विहार, शिल्परत्न, उत्तररामचरित, जैन ग्रंथ नायधम्मकला में चित्रकला के संकेत हैं। विष्णुधर्मोत्तर पुराण में तो चित्रकला की विधिवत सांगोपांग व्यख्या ही उपलब्ध है।
प्रत्येक घर चित्र से अलंकृत होता था और उसकी भित्ति पर चित्र बने होते थे। भित्ति चित्र का इस देश में इतना अधिक प्रचार था कि भित्ति शब्द ही यहां चित्रों के आधार के लिए रूढ़ हो गया, जैसे यूरोप में चित्रों का आधार कैनवस समझा जाता है। चित्र तीन प्रकार के फलकों पर बनाए जाते थे। प्रथम फलक भित्ति या दीवार थी। दूसरा फलक धर्म या वस्त्र था और तीसरा फलक लकड़ी, तालपत्र, पत्थर और हाथी के दांत होते थे।
भारत में पुराने चित्रों के उदाहरण दीवारों पर मिलते हैं एवं उनकी अपेक्षा नवीन चित्र ताल पत्रों और कागज पर। भित्ति चित्र के जो उदाहरण भारत में उपलब्ध हैं, उनका वातावरण धार्मिक है। पहाड़ों को काटकर यहां चैत्य, विहार और मन्दिर बनाने की प्रथा थी एवं उन्हीं की दीवारों पर पलस्तर लगाकर चूने जैसे किसी पदार्थ की घुटाई करके उस पर चित्र बनाए जाते थे। ऐसी गुफाओं में सबसे प्राचीन जोगीमारा की गुफा है।
अजन्ता की गुफाओं के चित्रों के विषय बौद्ध धर्म से संबन्धित हैं। गौतम बुद्ध की जीवन घटनाएं, मातृ पोषक जातक, विश्वान्तर जातक, षडदन्त जातक, रूह जातक और महाहंस जातक आदि बारह जातकों में वर्णित गौतम बुद्ध की पूर्वजन्म की कथाएं, धार्मिक इतिहास तथा बुद्ध के दृश्य और राजकीय एवं लौकिक चित्र अंकित हैं।
अजंता के समान ही उदाहरण सिगिरिया (श्रीलंका) तथा बाध की गुफाओं में भी उपलब्ध हैं। दिनकर के अनुसार ’’अजन्ता, सिगिरिया और बाघ में जो चित्र उपलब्ध है, उन्हीं में हम भारतीय चित्रकला की परिणति के प्रमाण देखते हैं। बौद्ध धर्म के साथ-साथ भारत की संस्कृति और कला भी भारत के बाहर पहुंचने के कारण सीलोन, जावा, स्याम, बर्मा, नेपाल, तिब्बत, जापान, हिन्द चीन और चीन में भी भारतीय चित्रकारी के नमूने उपलब्ध हैं एवं उनके अध्ययन के बिना भारतीय कला का अध्ययन पूरा नहीं कहा जा सकता।
गुप्त काल के बाद से चित्रकला का धीरे-धीरे ह्रास प्रारंभ हो हुआ। पाल शासन में बने चित्र अपेक्षाकृत उत्तम कोटि के थे। दक्षिणापथ के चित्रों को देखें तो प्रारंभिक चित्रकला में जो मानव आकृतियां अथवा देवी-देवताओं के चित्र बनाए गए हैं, वे पूरी तरह वहां की विशेषताओं के अनुरूप वहां के आदिवासियों की शारीरिक बनावट वाली हैं।