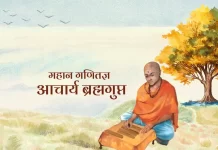Post Vedic period culture
Uttar Vaidic Kalin Sanskriti से तात्पर्य उस काल से है, जिसमें वेदों तथा सनातन ग्रंथों, अरण्यकों, उपनिषदों एवं महाकाव्यों की रचना हुई थी। उत्तर वैदिक काल की तिथि 1000 – 600 ईसवी पूर्व मानी जाती है। उत्तर वैदिक काल में आर्य सामाजिक जन जीवन, संस्कृति एवं राजनैतिक पटल पर भारी परिवर्तन आया। पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में प्रत्येक क्षेत्र में भारी परिवर्तन और प्रगति आयी।
Uttar Vaidic Kalin Sanskriti आर्यों के लिए प्रगति और विस्तार का काल था। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का विस्तार हिमालय से विंध्याचल तक हो गया था। इस काल की प्रमुख विशेषताएँ थी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कवायली संरचना में दरार का पड़ना और वर्ण व्यवस्था का जन्म तथा क्षेत्रगत साम्राज्यों का उदय। इस काल में लौह तकनीक ने क्रांतिकारी योगदान दिया।
उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था
Post Vedic Social System
उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों से तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर व्यापक प्रकाश पड़ता हैं। पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में आर्य सामाजिक पटल पर भारी परिवर्तन आया। वर्ण – व्यवस्था ने ठोस आकार ले लिया था। आश्रम व्यवस्था की स्थापना तथा शिक्षा की प्रगति एवं स्त्रियों की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन आया। उत्तर वैदिक काल में लोग ग्राम एवं नगरों दोनों में रहने लगे थे।
उत्तर वैदिक कालीन वर्ण – व्यवस्था
Post Vedic Period Varna System
उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन में ’वर्ण व्यवस्था’ का जन्म हुआ। पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में वर्ण में जबरदस्त परिवर्तन आया। अब यह समाज में पूर्णतः स्थापित हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल मे वर्ण, जन्म पर आधारित होकर पैतृक हो गया था। इस काल में चारों वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र) के कर्तव्यों एवं अधिकारों को स्पष्टतः परिभाषित कर दिया गया था।
ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों के लिए अंतिम संस्कार हेतु पृथक- पृथक स्थानों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल मे ’वर्ण’ कठोर होकर ’जाति’ का रूप ले चुका था। किन्तु फिर भी इस काल में जाति परिवर्तन समाज में मान्य था तथा विभिन्न जातियों में परस्पर विवाह भी हो जाते थे। वर्ण – व्यवस्था में इस काल में न तो पूर्व वैदिक युग के समान स्वतंत्रता थी और न सूत्रकाल की तरह के बंधन युक्त थी, यह दोनों के बीच की स्थिति थी।
ब्राह्मण वर्ण, पुरोहित वर्ग, शैक्षणिक अध्ययन-अध्यापन एवं धार्मिक क्रियाकलापों का कार्य करता था। क्षत्रिय वर्ण का कार्य राजकाज करना एवं प्रजा को सुरक्षा देना था। वैश्य वर्ण, कृषि एवं पशुपालन, विभिन्न व्यवसायों, व्यापार – वाणिज्य का कार्य करता था। शूद्र वर्ण का कार्य समाज के सभी की सेवा करना था। शूद्र वर्ण विभिन्न शिल्प कार्यों में भी संलग्न था।
उत्तर वैदिक कालीन समाज में भी अन्तर्जातीय विवाह, व्यवसाय परिवर्तन और सहभोज पर कोई नियंत्रण और प्रतिबंध नहीं था। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यकोपनिषद्, छान्दोग्य उपनिषद् आदि में शूद्र एवं चाण्डाल को भी यज्ञ की अनुमति दी गयी है। अतः सामाजिक एवं धार्मिक दोनों ही पृष्ठभूमि पर चारों वर्णों में समानता विद्यमान थी।
उत्तर वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था
Post Vedic Period Ashram System
उत्तर वैदिक कालीन समाज में एक आधारभूत सामाजिक परिवर्तन ‘आश्रम व्यवस्था’ के अस्तित्व के रूप में आया। भारतीय संस्कृति की आश्रम व्यवस्था विश्व के सामाजिक इतिहास एवं संस्कृति के लिए अद्भुत एवं अभूतपूर्व देन है। भारतीय मनीषियों ने अपने भौतिक चिंतन से आश्रम व्यवस्था के रूप में एक ऐसी व्यवस्था का सृजन किया। जिसमें व्यक्ति के जीवन का वैज्ञानिक विभाजन करके जीवन के प्रत्येक भाग का समुचित एवं सुनियोजित उपयोग का मूलमंत्र निहित था।
भारतीय मनीषियों की इस चिंतनशील व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान करना था। भारतीय मनीषियों ने बड़ी समझबूझ और योग्यता से व्यक्ति के जीवन का प्रबंधन किया तथा 100 वर्षों का जीवन काल मानकर 25 – 25 वर्षों के चार भागों (आश्रमों ) में विभाजित था और इस विभाजन की पृष्ठभूमि में प्रत्येक भाग की विशिष्ट उपयोगिता एवं विशेषता थी, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ समाज को मिलना था।
ब्रह्मचर्य – छात्रावस्था से 25 वर्ष तक, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष की आयु का तक, वानप्रस्य आश्रम 50 से 75 वर्ष तक, संन्यास 75 से 100 वर्ष तक का होता था। आश्रम व्यवस्था का दर्शन प्राचीन व्यवस्थाकारों के अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है, जिसमें ज्ञान और विज्ञान लौकिक और पारलौकिक, कर्म और धर्म तथा भोग और त्याग का अद्भुत समन्वय है।
उन्होंने जीवन की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए ज्ञान, कर्तव्य , त्याग और अध्यात्म के आधार पर मानव जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास नामक चार आश्रमों में विभाजित किया है, जिसका अन्तिम लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति।
उत्तर वैदिक कालीन परिवार
Post Vedic Period Family
उत्तर वैदिक कालीन समाज में परिवार ‘पितृ प्रधान’ एवं ‘संयुक्त परिवार’ की प्रथा थी। उत्तर वैदिक कालीन समाज में पिता के अधिकारों में वृद्धि हुई। वह अपने पुत्रों की उत्तराधिकार से वंचित रह सकता था। पुत्र, पिता की संपत्ति का स्वाभाविक उत्तराधिकारी होता था। संयुक्त परिवार में सभी स्त्री-पुरूष सान्नदित, समानता एवं सुमति के साथ रहते थे।
उत्तर वैदिक ग्रंथों में परिवार की ‘शांति एवं सुमति’ के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएँ की गयीं है। उत्तर वैदिक कालीन समाज मूलतः ’ग्राम प्रधान’ था। लोग कच्ची इंटों के घरों में या खम्भों पर टिके नरकुल और मिट्टी के घरों में रहते थे। यह छत घास – फूस और खर इत्यादि से पाटी जाती थी। फिर भी कतिपय उदाहरण नगरीय जीवन की ओर आर्य जीवन संस्कृति के बढ़ने के संकेत देते है।
उत्तर वैदिक कालीन विवाह
Post Vedic Period Marriage
उत्तर वैदिक कालीन समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में पुरूष के लिए यज्ञ, स्वर्ग, पूर्णता तथा पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु विवाह अत्यावश्यक था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में विवाह के आठ प्रकारों का उल्लेख मिलता है – ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह।
उत्तर वैदिक ग्रंथों में प्रथम चार प्रकार ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य को धर्मानुसार श्रेष्ठ एवं असुर, गांधर्व, राक्षस, पैशाच को अधार्मिक एवं निकृष्ट श्रेणी का माना गया हैं। रूत्री-पुरूष का विवाह युवा होने पर ही होता था। उत्तर वैदिक कालीन समाज में भी ’एकपत्नी प्रथा’ आदर्श रूप में प्रतिष्ठित थी। हालाँकि, बहु – विवाह तथा बहु पत्नी प्रथा भी समाज में विद्यमान थी।
बहु – विवाह तथा बहुपत्नी प्रथा संभवतः प्रशासनिक और राजकीय वर्गों में प्रचलित थी। समाज में पुनर्विवाह, विधवा विवाह तथा नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। अनुलोम-प्रतिलोम, सजातीय एवं अन्तर्जातीय विवाहों के उल्लेख मिलते हैं।
उत्तर वैदिक कालीन स्त्रियों की स्थिति
Status of Women in the Post Vedic Period
उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों से विदित होता है कि, उत्तर वैदिक काल में स्त्री की स्थिति अच्छी थी। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों अथर्ववेद (1.2.3), शतपथ ब्राह्मण (1.19.2.14), तैत्तिरीय ब्राह्मण (3.75) आदि में वर्णित है कि, स्त्री अपने पति के साथ याज्ञिक कार्य में अनिवार्य थी अर्थात् पत्नि के बिना कोई याज्ञिक और धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं हो सकता था तथा स्त्री – पुरुष दोनों को यज्ञ रुपी रथ के जुड़े हुए दो बैल की संज्ञा दी गई थी।
उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों अथर्ववेद (2.36.1, 11.1.17), शतपथ ब्राह्मण (5.1.6.10, 5.2.1.10) एवं ऐतरेय आरण्यक (1.2.5) में वर्णित है कि, स्त्री के बिना पुरुष अपूर्ण है, स्त्री के बिना पुरुष यज्ञ का अधिकारी नहीं है, और न ही स्वर्ग जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक – धार्मिक कृत्यों में स्त्री का अत्यधिक महत्व था। इस काल में स्त्री की चर्तुमुखी शिक्षा – दीक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था।
अथर्ववेद (11.5.18) में वर्णित है कि, शिक्षित स्त्री – पुरुष का विवाह उत्तम एवं श्रेष्ठ होता है। अतः इस युग में शिक्षित स्त्री – पुरुष का विवाह अच्छा माना जाता था। मैत्रायणी संहिता (3.7.3) में स्त्रियों की संगीत – नृत्य में रुचि का वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण (14, 3.1.35) सामगान को स्त्रियों का विशेष कार्य बताया हैं। इससे स्पष्ट है कि, स्त्रियाँ संगीत, नृत्य, गायन में प्रवीण होने के साथ – साथ मंत्रों की भी अच्छी ज्ञाता थी।
बृहदारण्यक उपनिषद् (3.6.8, 2.4.3, 4.5.4) में वर्णित है कि, जनक की सभा में गार्ग्री – याज्ञवल्क्य संवाद एवं मैत्रेयी द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु समस्त संपत्तिधिकार त्याग दिया था, यह स्त्रियों के ज्ञानवती एवं विदुषी होने का प्रतीक है। बृहदारण्यक उपनिषद, (3.6) में वर्णित है कि, सामाजिक और धार्मिक उत्सवों, समारोहों में स्त्रियाँ अलंकृत होकर बिना किसी प्रतिबंध के उन्मुक्त होकर हिस्सा लेती थी।
अथर्ववेद (6.5.27-29) के उल्लेखों से विदित है कि, इस काल में भी नियोग प्रथा प्रचलित थी तथा विधवा को पुत्र प्राप्ति का अधिकार था। इस काल में स्त्रियों के राजनैतिक अधिकारों में कुछ कमी आयी, किन्तु यह भी सत्य है कि, राजसूय यज्ञ के दौरान जिन लगभग एक दर्जन ‘रत्निनो’ के घर राजा जाता था, उनमें से चार स्त्रियाँ होती थी।
किन्तु यह भी सत्य है कि, ‘सभा’ में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में कमी के प्रमाण मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में कमी आयी। सती प्रथा इस युग में प्रचलित नहीं थी।
उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों मे स्त्रियों की अच्छी स्थिति के अधिक साक्ष्य उपलब्ध है। पुत्री के जन्म को हर्सोल्लास के साथ मनाने के अनेक वृतांत उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों मे उपलब्ध है। बृहदारण्यकोपनिषद् में धीमती कन्या के जन्म के निमित्त विधि – नियम बताये गये हैं। उत्तर वैदिक काल मे स्त्रियों को सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक अधिकार प्राप्त थे।
उत्तर वैदिक कालीन मनोरंजन के साधन
Means of Entertainment in the Post Vedic Period
उत्तर वैदिक कालीन समाज में आर्य सुखी – आनंदित जीवन के लिए उन्मुक्त होकर अनेक प्रकार के मनोरंजन के साधनों का उपयोग करते थे। रथदौड़, घुड़दौड़, आखेट, द्यूत, नृत्य, गान एवं संगीत आदि आर्यों के मनोरंजन के साधन थे। उत्तर वैदिक ग्रंथों में रथदौड़ एवं घुड़दौड़ के विजेताओं को इनाम देने के प्रमाण मिलते है।
उत्तर वैदिक कालीन समाज में मनोरंजन के साधनों में नाटकों का प्रसार तेजी बढ़ा होगा। क्योंकि, उत्तर वैदिक ग्रंथों में ‘शैलूष’ (नाटक के पात्र) तथा ‘शत तंतु‘ (सौ तारों वाली वीणा) का उल्लेख सार्वजनिक महोत्सवों पर नाटक में सौ तारों वाली वीणा पर गाथाओं को गाने के प्रमाण मिलते है।
उत्तर वैदिक कालीन खानपान
Post Vedic Period Food
उत्तर वैदिक कालीन समाज में भी आर्य मूलतः शाकाहारी थे। उत्तर वैदिक कालीन समाज में आर्य शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन किया जाता था। किन्तु उत्तर वैदिक कालीन समाज में मांसाहार पर बड़ा परिवर्तन आया। क्योंकि, इस काल में मांस खाना बुरा माना जाने लगा था। शाकाहारी भोजन में दूध, दही, मक्खन, घी, शहद, गुड़, चीनी, दूध से बनी खीर, फल और सब्जियाँ आदि का प्रयोग किया जाता था।
उत्तर वैदिक कालीन समाज में सुरापान अधिक प्रचलित हा गया था, किन्तु उत्तर वैदिक ग्रंथों में सुरापान को एक बुराई के रूप में वर्णित किया गया है। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का भी सर्वाधिक प्रिय पेय ’सोमरस’ था।
उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा
Post Vedic Period education
उत्तर वैदिक कालीन समाज में एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन शिक्षा के तेजी से प्रसार – प्रचार रूप में आया। उत्तर वैदिक काल में लेखन कला के अस्तित्व में आने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर समाज अग्रसर हुआ। उत्तर वैदिक काल में ’उपनयन संस्कार’ का उल्लेख मिलने लगता है। उत्तर वैदिक कालीन समाज में भी शिक्षा राज्य का दायित्व नहीं था। शिक्षा गुरूकुलों, गुरूग्रहों, आचार्यकुलों में दी जाती थी।
अथर्ववेद में शिक्षा का उद्देश्य श्रद्धा, मेधा, प्रज्ञा, धन, आयु, मोक्ष प्राप्ति बताया है। धार्मिक एवं साहित्यिक शिक्षा के साथ – साथ अस्त्र – शस्त्रों की युद्ध विद्या भी दी जाती होगी। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों के अतिरिक्त क्षत्रियों ने भी शिक्षादान प्रारंभ कर दिया था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में हम अनेक तत्वज्ञानी, दार्शनिक एवं ब्रह्मज्ञानी क्षत्रियों का उल्लेख पाते है।
शिक्षा सभी स्त्री एवं पुरूष समान रूप से प्राप्त करते थे। शिक्षा सभी वर्णों के लिए समान रूप से खुली हुई थी। फिर भी हमें उत्तर वैदिक कालीन समाज के परिवर्ती समय में शिक्षा में वर्ण विभेद के प्रमाण मिलने लगते है।
उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति
Economic Condition of Post Vedic Period
उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के आर्थिक जीवन की पृष्ठभूमि पर भारी परिवर्तन और प्रगति आयी। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था स्थापित हुई। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में लौह तकनीक ने क्रांतिकारी योगदान देना प्रारंभ किया। लोग बड़े- बडे़ ग्रामों और नगरों में रहने लगे। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के आर्थिक जीवन में लघु उद्योग एवं व्यापार – वाणिज्य ने भी महत्वपूर्ण योगदान देना प्रारंभ किया।
उत्तर वैदिक कालीन कृषि एवं पशुपालन
Agriculture and Animal Husbandry of the Post Vedic Period
उत्तर वैदिक कालीन आर्यों आर्थिक जीवन एक बहुत बड़ा परिवर्तन यह आया कि, कृषि प्रमुख व्यवसाय बन गया था। उत्तर वैदिक काल में गेहूँ, जौ, चावल, उड़द, मूंग, तिल, गन्ना आदि की फसल होती थी। अतरंजीखेड़ा से जौ, चावल, गेहूँ, तथा हस्तिनापुर से चावल एवं गन्ने के अवशेष मिले हैं। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का लम्बा वर्णन आया है। अथर्ववेद में हल को प्रवीरवंत (पवीरव) कहा गया है।
विद्वानों के अनुसार, लकड़ी के फाल वाले हल से जुताई होती थी। शतपथ ब्राह्मण मे जोतने को ‘कर्षण’ बोने को ‘वपन’ काटने को ‘कर्तन’ माड़ने को ‘मर्दन’ शब्द व्यवहार में मिलता हैं। दात्र (सृणि) अर्थात् दराँती के अवशेष अतरंजीखेड़ा से प्राप्त हैं। काठक संहिता में हल जोतने के लिए 6 से 24 बैलों का उल्लेख मिलता हैं। तैत्तरीय संहिता मे धान की कई किस्मों का उल्लेख है।
बृहदारण्यकोपनिषद् में 10 प्रकार के ग्रामीण अन्न का उल्लेख है। तैत्तरीय संहिता मे वर्ष में 2 बार तथा अष्टाध्यायी में तीन फसलों को उल्लेख किया है। उत्तर वैदिक कृषक कृषि में प्राकृतिक गोबर (शकृत, करीब), खाद् आदि उपयोग करते थे, उन्हें ऋतुओं का भी अच्छा ज्ञान था, जिसका उपयोग कृषि प्रक्रिया में करत थे। जोकि तत्कालीन विकसित कृषि प्रणाली का द्योतक हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेखित है कि, ‘अन्न ही ब्राह्म है।’’ एवं ‘अन्न बहु कुर्वति तद व्रतम् अर्थात् ‘अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए, यही हमारा व्रत होना चाहिए।
अनावृष्टि, अतिवृष्टि, विद्युत्पात, कीड़े – मकोड़े और टिड्डियों के भय से निवारण हेतु अथर्ववेद में यंत्र – मंत्रों का उल्लेख मिलता है। छान्दोग्य उपनिषद ‘एक दुर्भिक्ष का उल्लेख करता है, जो टिड्डियों द्वारा किये गये कृषि – विनाश के कारण पड़ा था। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों आर्थिक जीवन में कृषि के साथ ही पशुपालन का भी महत्वपूर्ण स्थान था। गाय – बैंल, भैंस, भेड़ – बकरी, घोड़ा, हाथी, ऊँट, कुत्ता, सुअर, गधा आदि का पशुपालन किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में भी गाय को सर्वाधिक पवित्र एवं दैवीय माना जाता था।
उत्तर वैदिक कालीन लघु – उद्योग एवं व्यवसाय
Post Vedic Period Small Industries and Business
उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के आर्थिक जीवन में लघु उद्योग एवं व्यापार – वाणिज्य ने महत्वपूर्ण योगदान देना प्रारंभ कर दिया था। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में वस्त्र बुननेवाले, वस्त्रों को काटनवाले, सिलनेवाले, बुननवाले, वस्त्रों पर कढ़ाई करने वाले‘, वैद्य, धातुकमर्, कुम्हार, बढ़ई, चर्मकार या चमड़े का कार्य करने वाले, नाई, धोबी, मछुए, खेत बोने वाले, रस्सी बटनेवाले, धनुषकार आदि अनेक व्यवसायों का उल्लेख मिलता हैं।
उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में सोना, चाँदी, ताँबा, सीसा, रांगा, टीन, पीतल एवं लोहे का उल्लेख मिलता हैं। पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में धातुकर्म का व्यवसाय अधिक प्रगतिशील एवं उन्नत अवस्था में आ गया था। इस काल में लोगों ने धातु गलाकर उसका शोधन करके विविध उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में कुशलता प्राप्त कर ली थी। पंचविश ब्राह्मण के ‘वयत्री’ शब्द तथा शतपथ ब्राह्मण के ‘तद्वा एतत्स्त्रीणां कर्म यदूर्णा सूत्रम’ उल्लेख से स्पष्ट है कि, स्त्रीयाँ वस्त्र बुनने का कार्य करती थी।
वाजसनेयी संहिता में वस्त्रों पर कढ़ाई करने वाली स्त्रियों को ‘पेशस्करी‘ कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में ‘कुलाल चक्र’ का उल्लेख मिलता है, कुलाल (कुम्हार) व्यवसाय के बारे में सूचना मिलती है। वाजसनेयी संहिता में पुरूष भेद के संबंध मे अन्य छोटे – बड़े अनेक व्यवसायियों का उल्लेख किया गया है। इस काल में आर्य चाँदी का उपयोग करने लगे थे, अथर्ववेद मे रजत (चाँदी) तथा तैत्तरीय संहिता में ‘रजतहिरण्य’ का उल्लेख है।
उत्तर वैदिक कालीन व्यापार – वाणिज्य
Post Vedic Period Trade – Commerce
उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन में आंतरिक एवं वैदेशिक व्यापार का उल्लेख मिलता हैं। वाजसनेयी संहिता, तैत्तरीय ब्राह्मण आदि में ‘वणिज’ शब्द का प्रयोग ‘व्यापारी’ के अर्थ में हुआ है। अथर्ववेद में एक स्थान से दूसरे पर सामग्री ले जाने वाले व्यापारियों का उल्लेख है। साधारणतया व्यापार में विनिमय का माध्यम ‘वस्तु – विनिमय’ और ‘गाय’ प्रमुख थी। इस युग में निष्क, शतमान जैसे मुद्रा की सुविधाजनक ईकाइयों से व्यवसाय में उन्नति हुई।
उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में तौल की ईकाइयों कृष्णल, रक्तिका, गुंजा, पाद का उल्लेख मिलता हैं। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में ब्याज पर और उधार धन देने के मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि, लोग ब्याज पर और उधार धन लेकर व्यापार एवं व्यवसाय करते होगे। इस युग में व्यावसायिक संघों के संकेत मिलते है।
उत्तर वैदिक काल मे धार्मिक स्थिति
Religious status in the Post Vedic Period
उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्थिति में अत्यधिक परिवर्तन हुआ। पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में यज्ञों एवं अनुष्ठानों का अधिक महत्व बढ़ गया। उत्तर वैदिक काल में धर्म में दार्शनिक चिंतनशील विचारधारा एवं ज्ञान तत्व का महत्व स्थापित हुआ। इस युग में यज्ञादि का एक स्वतंत्र पंथ के रूप में विकास हुआ।
अश्वमेध, रायसूय, सोमयज्ञ, वाजपेय, अग्निष्टोम, पुरूषमेध आदि अनेक यज्ञ-अनुष्ठान उत्तर वैदिक कालीन धर्म के अभिन्न अंग बन चुके थे। उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों की विचारधारा ने कर्मकाण्डों पर गहरा आघात किया। मुण्डक उपनिषद में कहा गया है कि, ‘‘केवल कर्मकांडी मूर्ख है। यज्ञ के द्वारा संसार सागर से पार होना अनिश्चित है। उपनिषदों ने ज्ञान मार्ग का रास्ता दिखाया। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि, ‘‘ज्ञान के बिना यज्ञ करना भी मृत्यु के आवर्त में ही चक्कर लगाना है।
उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति
Post Vedic Period Political Situation
उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति में अत्यधिक परिवर्तन आया। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक पटल पर साम्राज्यवाद का विकास हुआ। इस काल में कबायली संगठन में दरार पड़ी तथा शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय हुआ। वैदिक लोग इसलिए सफल हुए कि, उन के पास लोहे के हथियार और अश्वचालित रथ थे। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्य की उत्पत्ति तथा राजा की दैवीय उत्पत्ति संबंधी विवरण दिए गये है।
ऐतरेय ब्राह्मण में राज्य, स्वराज्य, भौज्य, वैराज्य, महाराज्य और साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि, मध्य देश के राजा, ‘राजा’, पूर्व के राजा ‘सम्राट’, दक्षिण के ’भोज’, पश्चिम के ‘स्वराट्’ और उत्तरी जनपदों के शासक ‘विराट’ कहलाते थे। राजा पदानुसार विभिन्न यज्ञों को सम्पादित करते थे।
इस युग में राजा की अनिवार्यता एवं उसके दैवीय अधिकारों में वृद्धि हुई। अथर्ववेद के राजतिलकोत्सव मंत्र से स्पष्ट है कि, जनता राजा को चुनती थी किन्तु राजपद मुख्यतः वंशानुगत हो गया था। शतपथ ब्राह्मण में ‘पाटव चाक्रस्थापिति’ और ‘दुष्टऋतु पौंसायन’ नामक राजाओं का उल्लेख है। इनके पूर्वज 10 पीढ़ियों से राज्य कर रहे थे।
राजा के राज्याभिषेक में ‘रत्निनों’ की सहमति आवश्यक थी। अथर्ववेद में 5, शतपथ ब्राह्मण में 11, तैत्तिरीय ब्राह्मण में 12 राज निर्माताओं का उल्लेख है। राजा के पदाधिकारी ‘रत्निन’ कहलाते थे। पंचविश ब्राह्मण में रत्निनों को ‘वीर’ कहा गया है। ये रत्निन थे – सेनानी, पुरोहित, ग्रामणी, युवराज, महिषी, क्षत्ता या क्षत्रि (प्रतिहारी), सूत्र (राजकीय चारण, कवि या रथवाहक), अक्षवाप (जुए का निरीक्षक), पालागल (दूत), गोविकर्तन (आखेट में राजा का साथी), विकर्तन (राजा के साथ शतरंज खेलने वाला), संग्रहितृ (कोषाध्यक्ष), भागदूध (कर संग्रह करने वाला) आदि।
इस युग में ’सचिव’ नामक उपाधि का उल्लेख भी मिलता है। राजा सम्भवतः 1/16 आयकर लेता था। मजूमदार, प्रांतीय शासन की नियमित व्यवस्था का प्रारम्भ स्थापति और शतपति के वर्णन से माना जा सकता है। स्थपति का काम बाहरी क्षेत्रों का प्रबंध करना था, जिनमें बहुधा केवल आदिवासी बसते थे जबकि शतपति सम्भवतः सौ गाँवों के एक समूह की देखभाल करता था। शतपति – स्मृति ग्रथों में उल्लिखित ग्रामीण अधिकारियों की विशाल श्रंखला के पूर्वज थे। प्रश्न उपनिषद के उल्लेखानुसार, इन अधिकारियों में ‘ग्राम अधिकृत‘ सबसे निम्न स्तर पर थे, जिन्हें स्वयं राजा नियुक्त करता था।
उत्तर वैदिक कालीन सभा – समिति
Post Vedic Period Assembly – Committee
अथर्ववेद में सभा – समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है। अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों के वर्णनों से स्पष्ट है कि, इस काल में सभा – समिति की सम्मति के बिना राजा साधारणतया कुछ नहीं करता था। अथर्ववेद (5.19.15) में वर्णित है कि, राजा के लिए सबसे बड़ा श्राप यही था कि, उसे समिति का सहयोग प्राप्त न होना – ‘‘नास्मै समितिः कल्पते न मित्रं नयते वशम्।’’
उत्तर वैदिक कालीन न्याय – व्यवस्था
Post Vedic Period Justice System
उत्तर वैदिक काल में न्याय व्यवस्था में भी विकास हुआ। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। उत्तर वैदिक काल में न्याय व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों का उल्लेख मिलने लगते है। ‘स्थपति’ सम्भवतः न्यायाधीश होता था। ग्रामों में ‘ग्राम्यवादिन’ न्याय करता था। हत्या (मनुष्य) का दण्ड गाय देकर चुकाया जाता था। न्याय की ’दिव्य – प्रणाली’ प्रचलित थी। प्रमुख अपराध चोरी, डकैती, व्यभिचार, हत्या, धोखाधड़ी थे।