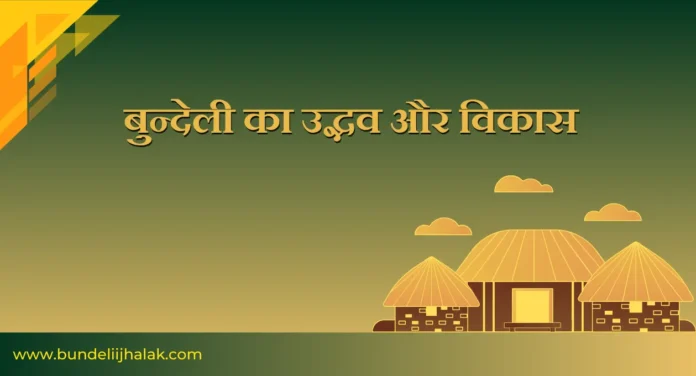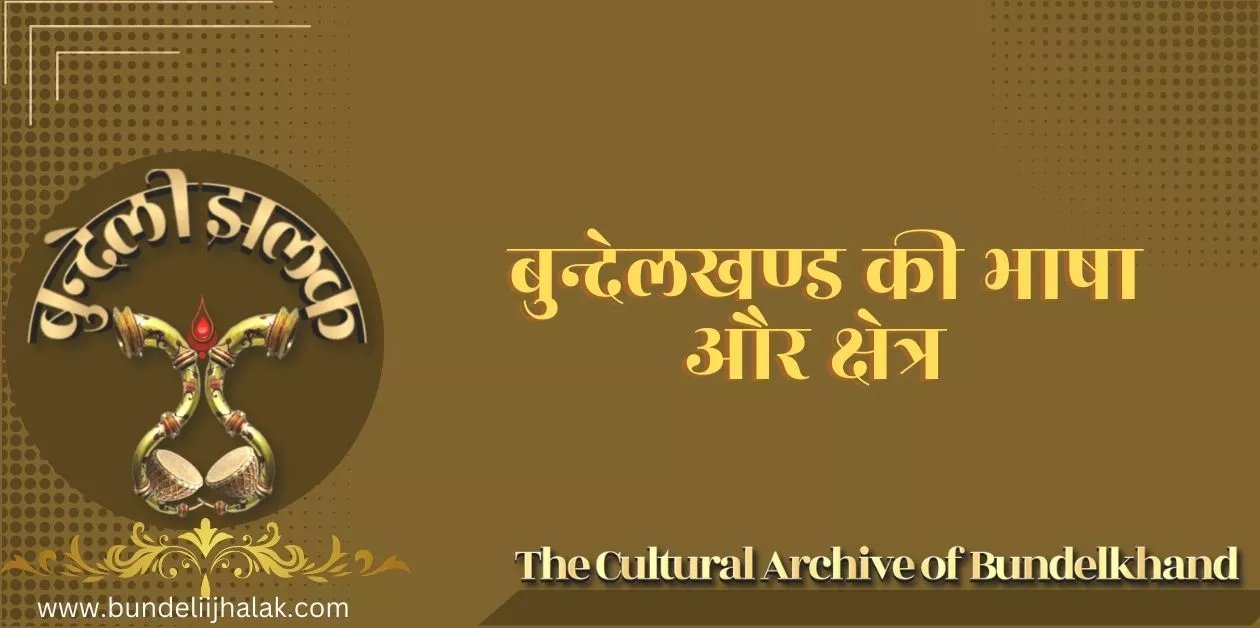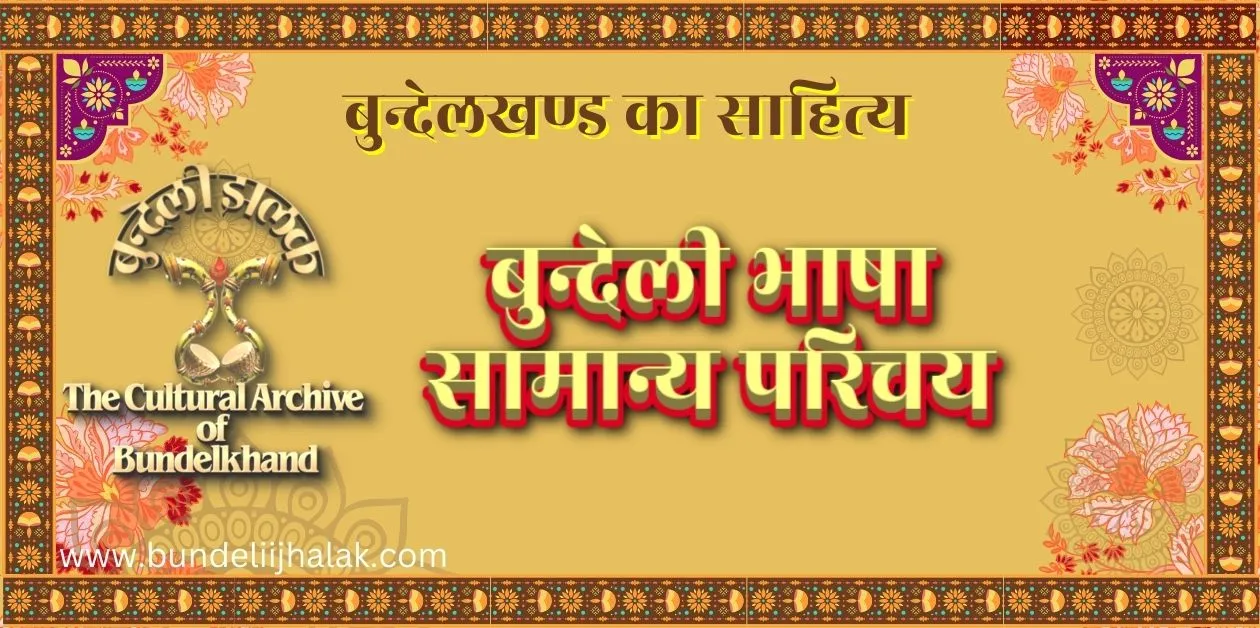बुन्देलखण्ड का अपना पौराणिक स्थान है। बुन्देलखण्ड में लोकभाषा में सृजन 11वीं शती से होने लगा था और बुन्देली का उद्भव और विकास 982 ई. या 10वीं शती के अन्तिम चरण मेे मानना उचित है। मौखिक परम्परा में प्रचलित “आल्हा” गाथा की रचना 12वीं शती के अन्तिम चरण में 1182 ई. के बाद और 1203 ई. के पूर्व हुई थी। ऐसे लोकगाथात्मक साहित्य का सृजन लोककाव्य की महानता को प्रमाणित करता है। 982 ई. या 10वीं शती के अन्तिम चरण से Bundeli ka Udbhav Aur Vikas मानना उचित है।

भारतीय संस्कृति (Indian Culture) का हृदय स्थल बुन्देलखंड मे Bundeli ka Udbhav Aur Vikas महाराज यशोवर्मन (लगभग 930 ई.) से वीरवर्मन (लगभग 1286 ई.) तक स्वतंत्रता, शक्ति और संस्कृति का प्रमुख केन्द्र था। चन्देलराज उत्तर में यमुना नदी से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में टोंस नदी से लेकर पश्चिम में चम्बल नदी तक फैला हुआ था, परन्तु उसका प्रभाव-विस्तार उत्तर में लगभग समस्त उत्तर भारत अर्थात् बंगाल से लेकर कश्मीर में सिन्धु के उदगम तक के तथा दक्षिण में चेदि से लेकर नर्मदा और चम्बल नदियों के तटीय क्षेत्र पर था।
यशोवर्मन (930-950 ई.) इतने शक्तिशाली थे कि कौशल राज्य, क्रथ राज्य, सिंहल राज्य तथा कुन्तल राज्य उसके निर्देश का पालन करते थे और गौड़, खस, कश्मीर, मिथिला, मालवा, चेदि, कुरू, गुर्जर आदि देशों पर उनका प्रभाव था। शक्ति में महाराज गंडदेव (950-1002 ई.) की तुलना शक्तिशाली हम्मीर से की गई है। गंडदेव (1002-1025 ई.) को तत्कालीन इतिहासकारों ने अपने समय का सर्व शक्तिशाली शासक माना है।
विद्याधर ने मुसलमानों से युद्ध में ऐसा शौर्य दिखाया था कि दो शताब्दियों तक मुसलमानों ने आक्रमण करने का साहस नहीं किया। कीर्तिवर्मन (1060-1100 ई.) ने भारतीय नेपोलियन चेदिनरेश कर्णदेव को पराजित किया, मदनवर्मन (1128-1164 ई.) ने प्रसिद्ध वीर जयसिंह सिद्धराज (1093-1143 ई.) को भी सन्धि करने के लिए विवश कर दिया और परमर्दिदेव (1165-1203 ई.) ने भी धारा, गढ़ा, अन्तर्वेदि, मालवा तथा पंजाब का कुछ भाग जीत लिया था। इससे साबित होता है कि चन्देल राज्य राजनीतिक दृष्टि से शक्ति का महत्वर्पूण केन्द्र था।

चन्देलों की शक्ति राजनीतिक दूर-दृष्टि के कारण इतनी अच्छी थी। उनकी राजनीति में शासन-व्यवस्था की मजबूती और विदेशी नीति में राष्ट्रीय एकता का विशेष महत्व था। उस समय राजपूत राज्य की सत्ता राजतन्त्र पर आधरित थी। राज्य की शक्ति मूलतः सामन्तों और उनके द्वारा नियुक्त सेना पर निर्भर थी। लेकिन चन्देलों की शासन-व्यवस्था में राज्य की सेना और सैन्य नीति पर अधिक ध्यान दिया जाता था।
उसके लिए अलग से सैनिक व्यवस्था थी, जिसके अन्तर्गत राज्य की स्थाई सेना और उसके पदाधिकारी तथा नगर की स्थाई सेना एवं अधिकारीगण आते थे। बड़े युद्धों में सामन्तों को अपनी सेना के साथ आकर लड़ना पड़ता था। तात्पर्य यह है कि सामन्त का विरोध राज्य के लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं कर पाता था। दूसरी प्रमुख बात यह थी कि चन्देल सेना में राजभक्ति के साथ राष्ट्रभक्ति की भावना प्रचुरता से भरी थी।
इसे भी देखिए: नमामि नर्मदे – चिरकुंवारी नर्मदा
गृह शासन के अन्तर्गत एक सुव्यवस्थित शासन का विवरण चन्देल शिलालेखों, तत्कालीन ग्रन्थों और ऐतिहासिक महत्त्व के उल्लेखों में उपलब्ध है। उनके अनुसार पूरा राज्य मंडलों में, मंडल विषयों में, विषय ग्राम समूहों में और ग्राम समूह कई ग्रामों में विभक्त था। इस तरह शासन की इकाई ग्राम था जिसका प्रबन्ध महत्तर अथवा मुखिया करता था। नगर की व्यवस्था पौर-बलाध्यक्ष के हाथ में थी, जो सुरक्षा के लिए सेना की टुकड़ियाँ भी रखता था।
नगरों का शासन विषयपति के नियन्त्रण में रहना उचित जान पड़ता है। ग्राम आत्मनिर्भर थे और उनमें रक्षक, दूत, वैद्य, ज्योतिषी, मेदु चांडाल आदि रहते थे। विषयपति और मंडलाधिपति की नियुक्ति राजा स्वयं करता था, जबकि अन्य की नियुक्ति विषय और मंडल के शासकों के अधिकार में थी। परमर्दिदेव के सेमरा लेख में तीन विषयों का भी उल्लेख है।
समस्त शासन का सूत्र राजा के हाथ में था। जो मंत्रिपरिषद और अधिकारियों की सहायता से शासकीय कार्यों का संचालन करता था। राजा के बाद उसकी पटरानी अथवा युवराज राजकाज सँभालते थे। मन्त्रियों के विभाग राजा की इच्छा से निश्चित होते थे। चन्देल अभिलेखों से न्याय, माल, सन्धि-विग्रह, धर्म, भांडागार के विभागों के उल्लेख मिलते हैं।
प्रत्येक विभाग एक अमात्य को सौंपा जाता था, जो उसके लिए राजा के प्रति जिम्मेदार होता था। कभी-कभी महामात्य या योग्य अमात्य को कई विभाग दे दिए जाते थे, संक्षेप में, राजा, अमात्यों और अधिकारियों और विभागीय तालमेल ने शासन की व्यवस्था को सुदृढ़ बना दिया था। चन्देलों की शासन-व्यवस्था आदर्श थी। वे जितने दृढ़ थे, उतने ही उदार थे। उनके पूरे इतिहास में निरंकुशता का कोई उदाहरण नहीं मिलता। सर्वत्र समृद्धि एवं शान्ति थी।

चन्देलों की विशेषता उनकी राष्ट्रीय चेतना थी। महाराज घंग ने सन् 990 ई. के लगभग सुबुक्तगीन के विरुद्ध प्रथम हिन्दू राज्यसंघ बनाया, जिसमें दिल्ली, अजमेर, कालिन्जर और कन्नौज के राजा सम्मिलित हुए। गंड ने सन् 1008 ई. में द्वितीय हिन्दू राज्य-संघ का संगठन किया और उसका नेतृत्व किया। गंडदेव की राष्ट्रभावना इतनी प्रखर थी कि जब कन्नौज के सम्राट ने तुर्क आक्रमणकारी महमूद के समक्ष आत्मसमर्पण करके देश के सम्मान को धक्का पहुँचाया।
कन्नौज के सम्राट को दंडित करने के लिए उसने अपने आत्मज विद्याधर को विशाल संघ-सेना के साथ भेजा। इतना ही नहीं राज्य की जनता ने भी राष्ट्रीय चेतना का प्रतिनिधित्व किया। हिन्दू वीरांगनाओं ने अपने जवाहरात बेच डाले इस धर्म युद्ध के संचालन के लिए उन्होंने दूरस्थ प्रदेशों से भी अपनी सहायता भेजी। स्पष्ट है कि चन्देल राज्य में राष्ट्र-भावना का अभाव नहीं था और उसने ही सबसे पहले राष्ट्रीय रक्षा का पवित्र कार्य किया था।

समाज में सभी वर्ण उपजातियों में विभाजित होने लगे थे, फिर भी ब्राह्मण, सामाजिक प्रतिष्ठा में ऊंचे माने जाते थे। चन्देल शिलालेखों के अनुसार कई मन्त्री ब्राह्मण थे। चन्देलों के राज्यकाल के प्रारम्भ में तो समाज के प्राचीन मर्यादाएँ बनी रहीं, पर उत्तरकाल में विघटन प्रारम्भ हो गया। तुर्कों के आक्रमणों से समाज में रूढ़िवादिता आदि अनेक दुर्बलताएँ आने लगी थीं। इस काल में क्षत्रियों का महत्त्व अधिक था। प्रशासन, युद्ध और रक्षा उनका दायित्व था।
परमर्दिदेव के अमात्य वत्सराज ने आदर्श क्षत्रिय को दानी, वीर और रसिक होना आवश्यक बताया है। लेकिन अधिकतर क्षत्रियों में बदला लेने, सम्पत्ति लूटने, कन्या का अपहरण करने और युद्ध लड़ने की प्रवृत्तियाँ थीं। चन्देल राजाओं की मान्यता थी कि विवाह एक सम-कुलशील वाले क्षत्रिय से हो।
राजा और क्षत्रिय अपनी कन्याओं को किसी से विवाहित करने में अपनी मानहानि अनुभव करते थे। मुगलों के सम्पर्क के कारण यह मनोवृत्ति और भी फैली। विवाहों को लेकर झगड़े और युद्ध भी हुए। इस परिस्थिति में कन्या अभिशाप समझी जाने लगी। ‘प्रबोध चन्द्रोदय’ में नारी को दुष्टा, विलासिनी, ईर्ष्यालु और शंकालु कहा गया है, पर सम्भवतः नाटककार ने धर्म-विमुखता के साधन रूप में स्त्री की दुर्बलताओं का संकेत किया है।
समाज में सामाजिक उत्सवों, धार्मिक कार्यों, त्यौहारों और विविध संस्कारों के लिए विभिन्न रीतियाँ थीं और उनका पालन सभी करते थे। हिन्दू आतिथ्य-सत्कार में सबसे आगे थे। सामाजिक विनोदों में अभिनय, नृत्य आदि प्रमुख थे। इस युग में नारी को सम्मानित पद प्राप्त था।
रमणियों (सुंदरियों / देहसुख देने वाली) के केश स्पर्श केवल प्रणय में ही किए जाते थे। अर्थात राज्य-प्रबन्ध इतना उत्तम था कि नारियाँ बिना किसी भय के स्वतन्त्रता का एहसास करती थी। वे सामाजिक कार्यों में भाग लेती थीं। इतिहासकार अलबरूनी का कथन है कि प्रत्येक पारिवारिक व्यवस्था और असाधारण स्थितियों में स्त्रिायों का परामर्श बड़ी निष्ठा से लिया जाता था। उनकी राय का महत्त्व होता था। उन्हें शिक्षा दी जाती थी।
प्रसिद्ध इतिहासकार टॅड ने आल्हा- उदल की माँ देवलदे की प्रशंसा में लिखा है कि विश्व के इतिहास में देवलदे की श्रेष्ठ और उदार देशभक्ति की तुलना में किसी स्त्री का उदाहरण नहीं मिलता। इसके साथ-साथ नारी पति के सुख-दुख में संगिनी होती थी। इतना ही नहीं, नारी पति की मत्यु पर सती होती थी। बुन्देलखंड में सती-स्तम्भों की अधिकता से सत्ती-प्रथा का प्रचलन सिद्ध हो जाता है।
चन्देल नरेश परमर्दिदेव के राज्य-काल (1165-1203 ई.) में नारी को सम्मानजनक स्थान नहीं मिला था। अमात्य वत्सराज द्वारा रचित रूपकों में उस समय की स्त्रिायों की दशा का चित्रण मिलता है। उसके वर्णनों के अनुसार स्त्री काम-वासना की साधन थी। कन्याओं का बलात् अपहर और कारण स्वरूप युद्ध अक्सर होता था। इसे शौर्य का प्रतीक माना जाता था। इस कारण कन्या का जन्म सुखद नहीं था। वह जन्म से लेकर पूरे जीवन भर एक दासी की तरह परतन्त्र रहती थी। स्पष्ट है कि वत्सराज का रूपक ‘रुक्मिणि हरण’ नारी की हरण-व्यवस्था का प्रतीक था।

धार्मिक दृष्टि से भी चन्देल राज्य की स्थिति समृद्ध थी। चन्देल नरेशों ने वैष्णव और शैव दोनों सम्प्रदायों को राजाश्रय प्रदान किया था। पराक्रमी यशोवर्मन बड़ा धर्मात्मा था, उसने खजुराहों में बैकुंठ मन्दिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो, महोबा, तथा अन्य स्थानों में विष्णु मन्दिर बनवाए गए, जिनमें विभिन्न अवतारों को भी महत्त्व मिला।
परवर्ती चन्देल नरेश शैव थे और उन्होंने अनेक शिवमन्दिरों की प्रतिष्ठा की, जिनमें खजुराहो का कन्दरिया, विश्वनाथ, मृत्युंजय, महादेव, नीलकंठ आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। उन्होंने शैव होते हुए भी कट्टर शैवों और कट्टर वैष्णवों की एकता पर ध्यान दिया। शक्ति-पूजा और उपासना का विकास दुर्गा, काली, शारदा देवी के मन्दिर तथा चैंसठ योगिनी, मनिया देवी के मन्दिरों से स्पष्ट है। सूर्य-पूजा का भी प्रचार था।
महोबा से प्राप्त उत्कृष्ट बौद्ध मूर्तियाँ यह सिद्ध करती हैं कि प्रारम्भ में बौद्ध धर्म उत्कर्ष पर था, किन्तु हिन्दू धर्म के प्रचार से वह पनप न सका। खजुराहो, दोनी, चाँदपुर, कुन्दनपुर आदि स्थानों के जैन मन्दिर चन्देलयुग में जैन धर्म की उन्नति के साक्षी हैं। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि चन्देल नरेशों में धार्मिक सहिषुणता थी और धार्मिक कलह या संघर्ष की समस्या नहीं थी। सभी सम्प्रदायों को समान सम्मान प्राप्त था।
शिव और विष्णु के मन्दिरों के बगल में जैननाथ और पाश्र्वनाथ के मन्दिर बनाने की स्वतन्त्राता थी। इससे सिद्ध है कि पूरे भारत में चन्देल-प्रदेश ही ऐसा भूभाग था, जिसमें सभी धर्मों को स्वतन्त्राता और सम्मान प्राप्त था तथा जिसने धर्म की वास्तविकता को समझा और धार्मिक एकता को सुरक्षित रखा। धार्मिक एकता की शक्ति के फलस्वरूप ही बुन्देलखंड पर इस्लाम का प्रभाव नहीं पड़ सका। मन्दिरों का विनाश हुआ, पर धर्म परिवर्तन की समस्या नहीं आई।
परमर्दिदेव के समय रचित वत्सराज के रूपकों में भी शिवपरक स्तुतियों से शैव धर्म की प्रधानता सिद्ध होती है, क्योंकि ‘समुद्रमन्थन’ में ‘विष्णु और ‘लक्ष्मी’ तथा ‘रूक्मिणी हरण’ में ‘‘मुरारिकृष्ण’’ की स्तुति से शैवों और वैष्णवों के बीच स्थापना का संकेत मिलता है। धार्मिक सहिशुण्ता चन्देलों का भूषण थी।
वत्सराज के रूपकों में दान महत्त्व की स्वीकृति रही है। उनके मत में राजा को दानी होना चाहिए। दान से दोषों का शमन होता है। धार्मिक कर्मकांड भी अधिक प्रचलित थे और लोग उन्हें अधिक महत्त्व देते थे। स्त्रिायाँ धार्मिक कृत्यों का अनुसरण-पालन करने में अग्रणी थीं, उनके कारण ही विजातीय आक्रमणों से रक्षा हो सकी।

चन्देल-काल में ललित कलाओं की उन्नति चरम सीमा तक पहुँच गई थी। वास्तुकला और मूर्तिकला के नमूने और उनकी विशिष्ट अभिव्यंजन पद्धति Specific expression method ने ललित कलाओं के इतिहास में एक नई दिशा का खोज की थी। खजुराहो की मूर्तियों में जहाँ जीवन और प्रकृति के विभिन्न रूपों को दर्शाया हुआ है, वहाँ उनका अंग-विन्यास, गठन, भंगिमा एवं अलंकरण, शिल्प के नए उपकरण प्रस्तुत करते हैं। मूर्तियों में कामुक मुद्राएँ जीवन के आनन्द में लीनता की प्रतीक हैं।
लौकिक आनन्द जो कि सूफियों की तरह आध्यात्मिक आनन्द की पहली सीढ़ी है। इन मूर्तियों के बाद एक साधु की आत्मानन्द में लीनता अंकित है, जो विकास की स्थिति का संकेत करती है। वास्तव में, कलाकार ने वासना के अभिप्राय के लिए भी विविध मूर्तियों को गढ़ा है, जिनसे दुर्बल मानव का चित्रण हुआ है और कहीं सबल मानव का।
मन्दिर के भीतर भी अकेली देव प्रतिमा आध्यात्मिक भावना का प्रतीक है। इस पर मन-मन्दिर का मनोवैज्ञानिक ढाँचा बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। मूर्तिकला में इन प्रतीकों एवं अभिप्रायों की निजी विशेषता है। स्थापत्यकला भी धर्म से प्रभावित है, चन्देलों के प्रासाद, बैठक, स्तम्भ, तड़ाग, दुर्ग का स्थापत्य उनके कौशल का प्रमाण है।
अभिनय-कला के विकास के कुछ प्रमाण मिलते हैं। महोबा के मदन सागर के बीच में एक रंगशाला निर्मित की गई थी, जिसके अवशिष्ट आज भी उसके वैभव की कहानी कहते हैं। ‘प्रबोध चन्द्रोदय’ नाटक कीर्तिवर्मन की कलचुरी कर्ण पर विजय के उपलक्ष में अभिनीत किया गया था। मन्दिरों के महामंडपों में अभिनय, नृत्य और संगीत के आयोजन होते थे। खजुराहो की मूर्तियों में संगीत और नृत्य के दृश्यों से तत्कालीन उन्नति का परिचय मिलता है।
स्पष्ट है कि चन्देल युग में सभी कलाओं का समानान्तर विकास हुआ है। उनमें कल्पना की सूक्ष्मता, भावना की सरसता और विचारों की प्रौढ़ता का अद्भुत समन्वय हुआ है और यह समन्वयवादी प्रवृत्ति भौतिक, दार्शनिक एवं धार्मिक दृष्टिकोणों में भी प्रकट होती है, जो चन्देलकाल की अपनी मौलिकता है।
इस युग में शिक्षा और साहित्य के विकास की खोज महत्त्वपूर्ण है। मन्दिर और अग्रहार ग्राम शिक्षा के केन्द्र थे तथा विद्वान ब्राह्मण विद्या की उन्नति के लिए प्रयत्नशील थे। विद्वानों को राज्य का संरक्षण प्राप्त था और विद्वत्ता के कारण उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। वेद, वेदांग, साहित्य, दर्शन आदि विषयों में उच्चशिक्षा की व्यवस्था थी। शिलालेखों में वेदांग के ज्ञाता ब्राह्मण अभिमन्यु, सूक्ति-रचनाकार राम साहित्य-रत्नाकर एवं श्रुतिपारदर्शन बलभद्र, कविचक्रवर्तिन नन्दन आदि का उल्लेख है। अभिलेखों की प्रशस्तियों से संस्कृत साहित्य के विकास का पता चलता है।

चन्देल नरेश परमर्दिदेव के समय चन्देल-चैहान संघर्ष एक ऐसी घटना थी, जिसने देश का इतिहास बदल दिया। दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चैहान ने वर्चस्व की होड़ में चन्देली शक्ति को सबसे अधिक बाधक पाया और फिर खोजा गया कोई बहाना। चन्देली सेना के वीरों आल्हा- उदल को राज्य से निष्कासन के फलस्वरूप कन्नौज में रहना पड़ रहा था, जो चैहानों के लिए सबसे अधिक लाभकारी अवसर था।
इस कारण पृथ्वीराज चौहान ने चन्देली द्वार (जहां से चंदेलों का राज्य शुरू होता है) सिरसा गढ पर आक्रमण कर दिया, फिर महोबा रणक्षेत्र बना और अन्त में बैरागढ़ का घमासान हुआ। कौन जीता, यह विवाद का विषय है, लेकिन इतिहासकारों का मत है कि चैहान विजयी रहे। दोनों पक्षों में सन्धि हुई, जिसके कारण चन्देल राज्य का कुछ भाग चैहानों का हो गया और चंदेलों की सीमा सिकुड़ गई।
सीमाएँ घटने-बढ़ने का निष्कर्ष उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है, जितना प्रसिद्ध इतिहासकार वि.वि. वैद्य का यह मत है कि ‘इसे एक ऐसी भूल समझनी चाहिए, जो राष्ट्रीय विनाश का कारण बनी’, क्योंकि तत्कालीन भारत के अग्रणी क्षत्रिय शासकों में एक थे।
तात्पर्य यह है कि पृथ्वीराज चौहान की राज्य बढाने की लालसा ने चन्देलों की उस शक्ति को तोड़ दिया जिससे विजातीय आक्रमणकारी भयभीत रहते थे। चन्देलों ने जिस राज्यसंघ के द्वारा राष्ट्रीय जागरण का कार्य किया था, उसे चैहानों ने पहचाना नहीं। जब राष्ट्र की रीढ़ ही टूट गई, तो फिर आक्रमणकारियों से सुरक्षित बचना मुश्किल था।

लोकभाषा /स्थानीय भाषा की उत्पत्ति परिस्थितियों, उसके आदिकालीन स्वरूप और विकास के इतिहास के सम्बन्ध में साहित्य के इतिहासकारों और भाषाविदों में कई भ्रान्तियाँ हैं। भारतीय संस्कृति और धर्म की गतिशीलता में ही लोकभाषा का उद्भव हुआ है। चन्देलों का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है। चन्देलों के राज्यकाल में बुन्देलखंड की सभ्यता और संस्कृति को न कोई नुकसान हुआ और न ही विजातीय संस्कृति का कोई प्रभाव पड़ा। दूसरी बात यह है कि बुन्देली भाषा का उद्भव (Origin of Bundeli language) मुगलों के प्रदेश पर अधिकार करने के पहले हो गया था।
इतिहासकार यह मान चुके हैं कि काशी, कन्नौज और महोबा के दरबारों में भाषा-कविता का बहुत सम्मान था। मुगलों का प्रभाव उसके बाद ही प्रारम्भ हुआ। इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश के उपरान्त हिन्दी की लोकभाषाओं का उदय अपनी भाषा-सम्बन्धी विशेष परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। एक भाषा जब अत्यन्त परिभाषित होकर शास्त्रीय और सीमाबद्ध हो जाती है, तो दूसरी भाषा तुरन्त विकसित होती है।
कला के उत्कर्ष में ग्वालियर तोमरकाल में एक प्रमुख केन्द्र था, जबकि मथुरा-वृन्दावन भक्ति और धर्म-भावना का केन्द्र था। जिस कला और साहित्य तथा उसके साथ भाषा का विकास ग्वालियर में हुआ, उसका धर्म में उपयोग मथुरा- वृन्दावन में हुआ ।
चन्देलों का राज्यकाल 9वीं से 13वीं शताब्दी तक पाँच सौ वर्षों की लंबी अवधि समेटे हुए है और इसी समय देशी भाषा का उद्भव और विकास हुआ। दूसरी बात यह है कि चन्देल साम्राज्य के अन्तर्गत लगभग पूरा मध्यदेश एवं दक्षिणी भारत का कुछ भाग सम्मिलित था। तीसरे चन्देलों ने इस मध्यदेश की संस्कृति को जहाँ एकता ,उन्नति और विस्तार दिया, वहीं कला को अपने आश्रय में विकसित कर एक ऊंचाई पर खड़ा कर दिया।
चंदेलो के शासन-काल में देशी भाषा का विकास जल्दी हुआ और इतना ही नहीं, वह साहित्य या काव्य की भाषा के रूप में भी शीघ्र प्रतिष्ठित हुई। यद्यपि पश्चिम में भदावरी, ब्रज और मालवा तथा पूर्व में बघेली बोलियाँ अपने स्वरूप धारण कर रहीं थीं, तब केन्द्र में बुन्देली का विकास हो चुका था। चन्देलों के राज्य की प्रमुख राजधानी महोबा, धार्मिक राजधानी खजुराहो और सैनिक राजधानी कालिन्जर थी।
ग्वालियर (गोपगिरि, गोपाद्रि) और मथुरा तक का प्रदेश चन्देलों के अधीन था। अतएव स्पष्ट है कि उस समय महोबा, खजुराहो और कालिंजर के क्षेत्र की भाषा ही साहित्य या काव्य-भाषा के पद की अधिकारिणी हुई और पूरे राज्य में उसी का प्रचार-प्रसार हुआ। बाद में मध्यदेश की संस्कृति का केन्द्र ग्वालियर बना, जहाँ इस भाषा का द्वितीय उत्थान हुआ।
भक्ति-आन्दोलन की चेतना से प्रभावित होने पर तीसरा केन्द्र मथुरा- वृन्दावन रहा, जहाँ इस भाषा को तृतीय उत्थान में एक व्यापक प्रसार मिला। इससे सिद्ध है कि बुन्देलखंड के दोनों केन्द्रों में लगभग 16वीं शताब्दी तक जो भाषा पल्लवित, पुष्पित और परिष्कृत होती रही तथा काव्य-भाषा के रूप में मान्य रही, वही मध्यकालीन काव्य की भाषा कही जा सकती है। इसलिए उसे मध्यदेशीय न कहकर बुन्देली मानना ही न्याय संगत है।
महाराज गंडदेव की 1023 ई. में देशी भाषा या बुन्देली में रचित एक कविता का उल्लेख इतिहास में मिलता है। जब 1023 ई. में बुन्देली भाषा में साहित्य की रचना होने लगी थी, तो यह निश्चित है कि उसके दो-डेढ़ सौ वर्ष पूर्व अर्थात 9वीं शती के प्रारम्भ में ही बुन्देली का प्रभाव हो गया था। दूसरे प्रदेशों से लगभग 2000 वर्ष पहले लोकभाषा के उदय का कारण यह भी हो सकता है कि चन्देलों के शासन-काल में 9वीं शती से ही एक परिवर्तन का प्रारम्भ होता है और चन्देलों के इतिहास में उन्नति का वास्तविक प्रारम्भ एवं नए युग का सूत्रपात 910 ई. से होता है।
यशोवर्मन से तो (930 ई.-950) एक व्यापक परिवर्तन उभर आता है। दूसरा कारण यह है कि बुन्देलखंड में बाहरी आक्रमणों का ताँता-सा लग जाता है, अतएव उन आक्रमनों से अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए लोकभाषा एक अनिवार्य माध्यम बन जाती है।
एक तो चन्देल नरेश महाराज धंग के काल में निर्मित जिननाथ का जैन मन्दिर का सं. 1011 (सन् 954 ई.) का अभिलेख है, जिसमें कुछ वाटिकाओं की भेंट का उल्लेख है। उनमें से एक वाटिका का नाम ‘‘धंगवारी’’ है। जिसमें वारी शब्द संस्कृत की वाटिका या वाटी के लिए प्रयुक्त हुआ है और वह लोकप्रचलित बुन्देली का ही शब्द है। इसी प्रकार अजयगढ़ के सं. 1243 (1186 ई.) के अभिलेख में ‘चैंतरा’ (चैत्रो) बुन्देली का प्रयोग है।
पुरातत्वविद कनिंघम ने अजयगढ़ के सं. 1269 (1212 ई.) की भाषा के सम्बन्ध में स्पष्ट लिखा है कि शिमला के पंडित द्वारा उसे संस्कृत नही कहा गया है, वरन् कोई हिन्दी की बोली बताया गया है। वस्तुतः उसकी भाषा संस्कृत न होकर तत्कालीन बुन्देली थी। इसी तरह सं. 1372 का अभिलेख संस्कृत में नहीं है। तात्पर्य यह है कि बुन्देली का उदय 954 ई. के पूर्व 9वीं शती में हुआ था, क्योंकि अभिलेखों में उन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है, जो मान्य हो जाते हैं। लोकभाषा में अभिलेखों की परम्परा निरन्तर गतिशील रही है।

बुन्देलखंड में काव्य का विकास कब से प्रारम्भ हुआ, यह निश्चित करना कठिन है और प्रारम्भिक -काल में उसका क्या स्वरूप था, यह निर्धारित करना तो और भी कठिन है। किन्तु इतना निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि हिन्दी में काव्य की रचना 11वीं शती से होने लगी थीं।
चन्देल नरेश महाराज गंडदेव (1002-1025 ई.) में 1023 ई. में चन्देलों और महमूद गजनवी के बीच सन्धि के समय सुल्तान की प्रशंसा में एक हिन्दी कविता भेंट की थी और उस कविता के भावों एवं भाषा से स्वयं सुल्तान तथा उनके साथ आए हुए कवि बड़े प्रभावित हुए थे।
गंडदेव ने एक वीर और दूरदर्शी शासक के रूप में 22-23 वर्षों तक राज्य-भार सँभाला और उसके राज्य के अन्तर्गत एक विस्तृत भूभाग था। पश्चिम में चम्बल नदी तक उसका अधिकार था। कच्छपात और ग्वालियर के शासक उसके करद थे। कन्नौज भी चन्दोलों के संरक्षण में था। दक्षिण का कलचुरी शासक भी उनसे पराजित हो चुका था।
चन्देलों की शक्ति का इतना प्रभाव था कि इतिहासकार गर्दिजजी ने लिखा है कि आक्रमणकारी सुल्तान महमूद भी एक बार भय से आक्रान्त हो गया था। गंडदेव की प्रमुख विशेषता यह थी कि उसने महमूद के आक्रमण के समय राष्ट्रीय संकट को पहचानकर द्वितीय हिन्दू-राज्य-संघ में प्रमुख योगदान दिया था।
इतिहासकार स्मिथ ने तो कालिंजर के राजा गंडदेव के स्वयं सम्मिलित होने का उल्लेख किया है। इससे सिद्ध है कि गंड के शासन-काल में राष्ट्रीय चेतना की जाग्रति और एकता की भावना थी। 1018 ई. में महमूद के कन्नौज के आक्रमण से भयभीत होकर भागने वाले कन्नौज-नरेश राज्यपाल को दंडित करने के लिए चन्देल नरेश ने राजकुमार विद्याधर को भेजा था।
स्वयं चन्देल नरेश ने कालिंजर में महमूद का सामना किया। यद्यपि वह पराजित हुआ, किन्तु मुगलों के आक्रमण का अवरोध केवल चन्देल ही कर सके। इसमें सन्देह नहीं कि चन्देलों ने जिस ऐतिहासिक शौर्य का परिचय दिया, उससे दो सौ वर्षों तक मुगलों को चन्देलों पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ।
महाराज गंडदेव के उपरान्त चन्देल नरेश परमर्दिदेव (1165-1203 ई.) हिन्दी के विख्यात कवि माने गए हैं। कालिंजर-शिलालेख (1201 ई.) के अन्त में उल्लेख है कि परमर्दिदेव ने भगवान मुरारि की स्तुति स्वयं लिखी थी। 13 वीं शती में रचित पाश्र्वदेव के ग्रन्थ ‘संगीतसमयसार’ से पता चलता है कि परमर्दिदेव मध्यदेशीय-संगीत-पद्धति में विख्यात थे।
पाश्र्वदेव ने इस ग्रन्थ में कश्मीर के राजा मातृगुप्त, धार के राजा भोज, अनहिलवाड़ के चालुक्य नरेश सोमेश्वर और महोबा के चन्देल नरेश परमर्दिदेव को प्रमाण रूप में किया है। इस लिये परमर्दिदेव ने हिन्दी में पद-रचना अवश्य की थी, क्योंकि संगीत के आचार्य को पद रचना में भी दक्ष माना जाता है। यह भी निश्चित है कि परमर्दिदेव के राजाश्रय में पद रचनाकार थे, किन्तु उनकी रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं।
बुन्देली लोकभाषा में लोकगीतों का लोकप्रचलन भी 11वीं शती से हो गया था। उनका आधार अपभ्रंश का लाड़ला छन्द दोहर और प्राकृत का गाहा था। सर्वप्रथम कथनशैली को केन्द्र में रखकर लोकगायकी के वे उदाहरण मिलते हैं, जो मानव की दैनिकचर्या से सम्बद्ध थे अथवा इष्टदेवता की भक्ति व्यक्त करते थे।
इस शैली की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति कारसदेव की गोटें थीं, जिनमें चरागाही लोकसंस्कृति का वास्तविक वर्णन मिलता है। दोहा को केन्द्र में रखकर दिवारी गीत, सखयाई फागें और उसकी लटकनिया को लेकर राई गीत प्रचलित हुए। ‘गाहा’ के आधार पर देवी गीत, राछरे और भक्तिपरक गाथाएँ रची गईं। चरागाही, ऐतिहासिक और वीरतापरक गाथाओं से इस युग को लोकगाथा-काल कहना अनुचित नहीं है।
मुक्तकों की परम्परा में संस्कारपरक, रक्षापरक और प्रेमपरक गीत अधिक लिखे गए, लेकिन परिस्थितियों के कारण वीररसपरक लोकगाथाओं की प्रधानता रही। ‘कारसदेव की गाथा’ में वीरता ही केन्द्रीय तत्त्व के रूप में महत्त्वपूर्ण रही है, लेकिन वह आल्हा गाथा की तरह सार्वजनिक नहीं हो सकी। जनकवि जगनिक भाट द्वारा रचित आल्हा गाथाएँ एक वीरगाथात्मक लोकमहाकाव्य का रूप ग्रहण कर लेती हैं, जिसे साहित्य के इतिहासकारों ने ‘आल्हखंड’ कहा है।
मौखिक परम्परा और विकसनशील Developing प्रवृत्ति के कारण उसमें अनेक क्षेपक (किसी कृति की समाप्ति के बाद का जोड़ा हुआ या बैठाना) भले ही जुड़ गए हों और उसके स्वरूप में परिवर्तन भले ही आ गया हो, परन्तु यह सत्य है कि 12वीं शती में रचित यह कृति बुन्देली लोकभाषा में लिखी जाने के कारण सर्वोपरि महत्त्व रखती है और उसी को हिन्दी का प्रथम ग्रन्थ मानना समुचित है। वस्तुतः अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त यह कृति और उसका रचयिता जगनिक, दोनों बुन्देली और हिन्दी की उपलब्धि है।
बुन्देली लोक संस्कृति
संदर्भ-
बुंदेली लोक साहित्य परंपरा और इतिहास – डॉ. नर्मदा प्रसाद गुप्त
बुंदेली लोक संस्कृति और साहित्य – डॉ. नर्मदा प्रसाद गुप्त
बुन्देलखंड की संस्कृति और साहित्य – श्री राम चरण हयारण “मित्र”
बुन्देलखंड दर्शन – मोतीलाल त्रिपाठी “अशांत”
बुंदेली लोक काव्य – डॉ. बलभद्र तिवारी
बुंदेली काव्य परंपरा – डॉ. बलभद्र तिवारी
बुन्देली का भाषाशास्त्रीय अध्ययन -रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल

सांस्कृतिक सहयोग के लिए For Cultural Cooperation