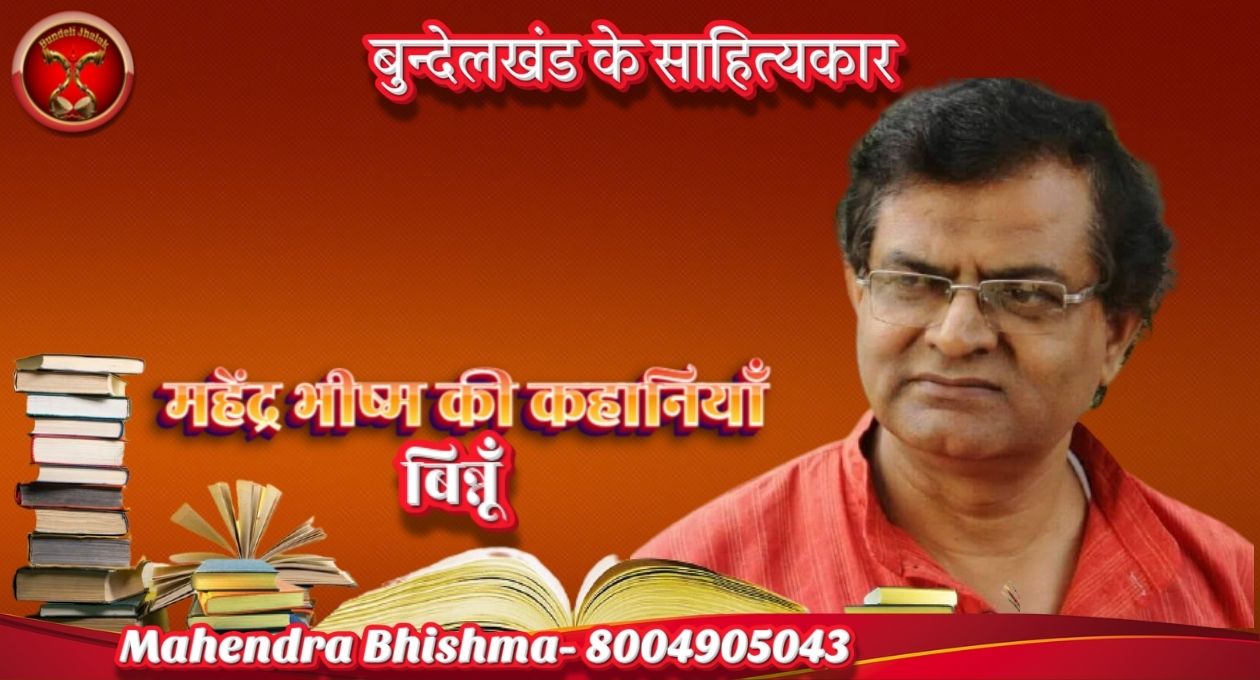वक़्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है ज़िंदगी कहानियों की तरह बनती-बिगड़ती रहती हैं। एक कहाँनी ही तो है। अल्हड आंधी की तरह थी Binnu ,उस बेल की तरह जो पेड की टहनी का सहारा मिलते ही लिपट जाती है। आज किस्मत ने बिन्नू को गाँव-भर की बूढ़ी बिनई काकी बना दिया ।
‘‘मोए रो लेन दो मराज्! मोखाँ रोए से न रोको……… सालन बाद इन आँखन से असुआं निकर रए…. ऊ बब्बा मरे हते, तब रोइती मैं। ऊके बाद आज जे असुआँ निकल रए …. मोरे जैसी अभागिन ई संसार में दूसरी कोऊ न हुए …… पैदा होतई मोरे बाप-मताई चल बसे, बूढ़े बब्बा ने पाल-पोस कर जवान करो, फिन मोरो ब्याओ करो, ब्याओ के चौथे रोज मोरो मड़ई करंट से चिपक के मर गओ, तबहूँ मोरी आँखन से असुआँ नई निकरे ते।
मोखाँ देवर के संगे बैठा दओ गओ। वो भी एक मोड़ा एक मोड़ी पैदा कराके ट्रैक्टर के तरे दब के मर गओ, तबहूँ मोरी आँखें नहीं पसीजी हती। मोड़ी अपने सासरे चली गई, तबहूँ न रोई मैं। मोड़ा ने अपनी लुगाई के कहे से मौखा घर से निकार कर, दर-दर की भिखारन बना दओ, तबहूँ मोरी आँखन से असुआँ नहीं टपके, पर मराज्! आज तुमाई जा दशा देख के, मोरो करेजो फटो जात। जे असुआँ रुके हाँ मानतई नइयाँ ….मराज्! मौसे जी-जी ने सम्बन्ध रखो। सबहाँ मौरी अभागिन सूरत ने विपदा में डारो … मैं बोत अभागन हो मराज!’’ बिन्नूँ रोए जा रही थी।
उम्र के अन्तिम पड़ाव में वह वर्षों बाद मुझसे आज मिली थी। आज से लगभग चालीस वर्ष पूर्व की चौदह-पन्द्रह साल की दुबली-पतली, तीखे नैन-नक्श वाली अल्हड़ बाला बिन्नूँ और आज गाँव-भर की बिनई काकी बन चुकी बिन्नूँ में जमीन-आसमान का अंतर आ चुका था। उसके खिचड़ी बाल, मोटा किन्तु कमजोर-सा शरीर, निस्तेज चेहरा, बुझी हुईं आँखें। आज से चालीस साल पहले वाली बिन्नूँ से एकदम अलग थी, मेरे पास बैठी गाँव भर की ‘बिनई काकी’।
मैं जब तक नौकरी में रहा, बीसियों तरह के लोग मेरे आगे-पीछे रहते थे, परन्तु नौकरी से रिटायर होने, फिर तुरन्त ही एक्सीडेंट से अपनी दोनों टाँगे खो देने के बाद मेरी जिंदगी धीरे-धीरे नरक बनती चली गयी। अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए मैं बोझ बन गया था। अपमान और तिरस्कारपूर्ण जिंदगी जीते रहना मेरी नियति बनती जा रही थी। अपने ही खून से पल-पल अपमानित होकर उनके द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार को सोचने मात्र से ही यह संसार बेमानी लगने लगता है। पद, प्रतिष्ठा और वैभवपूर्ण जीवन जीने वाले व्यक्ति को एकाएक परिस्थितिवश अपने दैनिक-कार्यक्रमों के निष्पादन में भी दूसरे के सहारे की जरुरत ने संसार के लोगों का स्वार्थी चेहरा सामने ला दिया।
अपने सगे-संबंधियों के स्वार्थपूर्ण व्यवहार और तिरस्कार से संसार में जीने की इच्छा मर जाती है और जिजीविषा की समाप्ति के बाद पल-पल का जीवन बोझ बनता जाता है। इस समय घुटन महसूस होती है, मन में आत्महत्या का विचार प्रबल होता जाता है। आत्महत्या करने से अच्छा है, आत्महत्या की परिस्थितियों और वातावरण को एकदम से छोड़कर कहीं दूर चले जाना।
और ऐसा ही मैंने किया। गाँव में अपनी पुश्तैनी जमीन, खण्डहर होता हवेलीनुमा मकान, जहाँ मेरा बचपन बीता था, मुझे उस नरक से खींच लाया। आत्महत्या के कटघरे से अपने आप को मुक्त कराकर मैं अपने गाँव की स्वतन्त्र और ताजी हवा में शेष जीवन जीने के लिए किसी को भी बताये बिना कल यहाँ चला आया था। गाँव के मेरे बचपन के तमाम हम-उम्र साथी और मेरे पिता के समय के जीवित बचे लोग मुझसे मिलने आये।
पिताजी के विश्वासपात्र पंडितजी, जो पिताजी के स्वर्गवास के बाद से सारी कृषि उपज और हवेली की देखरेख कर रहे थे, मेरे एकाएक गाँव आने पर प्रसन्न और आश्चर्यचकित हुए। मेरे अपाहिज होने और परिवार के दुर्व्यवहार पर उन्हें अत्यंत दुःख भी हुआ। उनसे भी ज्यादा दुःखी थी मेरे सामने बैठी बिनई काकी, मेरे बचपन के स्वर्णिम दिनों की बराबर की हिस्सेदार ‘बिन्नूँ’।
“मराज्! अब इते से जइयो न! मैं करो तुमाई उसार मोए तुमाए गाड़ी के डराइवर ने सब बता दओ….. तुम तनकऊ दुःखी न हो …… ऊने मोय जो भी ….. बताओ कि तुम सब कुछ बेंच-बाच के तीर्थन हाँ निकर जे हो …….. नई ……. तुमें, अब कहूँ भी जाए की तनकऊ जरूरत नईयाँ ……. तुमाई ई बिन्नूँ के रातन तुमें अब कोनऊ तरा की परेशानी न उठाने परहै। मैं जीवन-जियत तुमाई सेवा-उसार करों ….. अब मौरे मरे के बाद ही जा पे हो मराज्!’’ कहते-कहते बिन्नूँ हिचकियाँ लेती सुबकने लगी।
गाँव में अच्छी खेती और प्रतिष्ठा के बावजूद मेरे पिता ने अपने इकलौते पुत्र को नौकरी के आकर्षण के व्यामोह में डालकर मुझे शहरी जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। मुझे अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष कुछ हजार रुपये माहवार की गुलामी करके सीमित दायरे में बँधे रहकर बिताने पड़े। इन वर्षो में मुझे न केवल अपनी अभिरुचियों को दबाये रखना पड़ा, अपितु अपनी लाखों रुपये सालाना की उपज देने वाली कृषि भूमि के प्रबन्ध से भी वंचित रहना पड़ा।
जब तक पिताजी थे। सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा। उनके देहावसान के तुरन्त बाद माँ का भी स्वर्गवास हो गया था, तब पण्डितजी के बार-बार आग्रह करने के बावजूद मैं गाँव नहीं आया था। उस समय मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए शहर में पूर्णतया संतुष्ट था। मैंने तब यह सोचा भी नहीं था कि मुझे सदा के लिए गाँव में रहने के लिये आना पडे़गा।
गाँव भी अब पहले जैसा गाँव नहीं रह गया था, उपनगर बन चुका था। कच्चे घरों के स्थान पर ईट के पक्के मकान बन चुके थे। चाय-पान की दुकानों की बाढ़-सी आ चुकी थी। पहले जहाँ पर ढँग की कच्ची सड़कें भी नहीं थी, वहाँ अब डामर रोड पर बसें चलने लगी थीं। अधनंगे, फटेहाल लोगों की जगह रंग-बिरंगे कपड़े और पहले से ज्यादा खुशहाल लोगों का गाँव बन चुका था। मेरे बचपन के उस गाँव से अबके इस गाँव में बहुत सारे बदलाव आ चुके थे, ठीक बिन्नूँ की तरह। कुछ चीजें बूढ़ी हो चुकी थीं और कुछ बूढ़े से जवान हो रही थीं।
बिन्नूँ की हिचकियाँ थम रहीं थीं। मैं भी उसके अन्दर की सारी भड़ास निकल जाने देना चाहता था। मैंने उसे रोने से रोकने का प्रयास नहीं किया। ‘‘का बताओ मराज्! मोय तुम कबहूँ नहीं बिसरे …….. तुमें मोरो मन हमेशा याद करत रओ ………. तुमने हमाए पीछे का को का नहीं करो। तुमाओ एहसान हम मरतन-मरत न भूल पेहैं। काए मराज! तुम्हें हमाये बब्बा की याद है? …. कि बिसर गए वे?’’
बिन्नूँ ने मेरे मस्तिष्क के किसी कोने में बंद अतीत की किताब के पहले के पन्नों को टटोला था। एक तेज निःश्वास के साथ अतीत के पन्नों पर पड़ी गरदा बाहर निकल आयी। बिन्नूँ ने पास रखे थूकदान को मेरे मुँह के पास बढ़ाया। खाँसी स्वतः अगले पल रुक गयी।
ठंड जोरों की थी। मैंने बिन्नूँ को अपने सीने पर ब्राण्डी मलने को कहा। बहुत देर तक मौन वह मेरे सीने पर ब्राण्डी मलती रही। ब्राण्डी का एक पेग ले लेने के बाद मैं उनींदा हो चला। इसी अर्द्धनिद्रा की अवस्था में, मैं सोते-जागते अपने अतीत के उन दिनों में पहुँच गया, जब मैं बारह-तेरह वर्ष का निपट किशोर था।
गुरुजी मुझे पढ़ाकर जा चुके थे। नित्य की भाँति मैं हवेली के पिछवाड़े आ गया। जहाँ पर पहले से अकेले ही कटिया-मशीन पर परशू बब्बा जानवरों के लिए करबी काट रहे थे। हमारे खेतों में दिनभर काम करने के बाद वह गोधूलि के समय बैलगाड़ी पर करबी का बड़ा-सा गठ्ठर रखकर लाते, फिर कटिया-मशीन से उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर गाय, भैंसों के खाने के लिए चिरई पर डालते। इस प्रकार दिया-बत्ती के समय ही वह अपने घर जा पाते थे।
‘‘परशू बब्बा! हम भी कटिया मशीन चलायेंगे।’’ मैंने कटिया मशीन के पास खड़े होकर परशू बब्बा से आग्रह किया। ‘‘नई भैया! तुमाए बस की नइयाँ जा, तुम एक कुदई बैठके देखो!’’ परशू बब्बा ने कटिया मशीन चलानी रोक दी और सुस्ताने लगे। गले पर पड़ी साफी से माथे पर फैल चुकी पसीने की बूँदे पोंछने के बाद वह पुनः कटिया मशीन चलाने लग गये। ‘‘परशू बब्बा!’’ मैंने पुनः आग्रह किया। ‘‘मान जाए करो। मैंने केदई न तुमाए बस की नईयाँ जा।’’ थकान से हाँफते-हाँफते परशु बब्बा बोले। हाँफने से उनकी आवाज कुछ तेज हो गई थी। ‘‘नहीं, हम चलाऐंगे।’’ मेरे शब्दों में विनम्र हठ था।
‘‘अच्छा! बहुतई जिद्दी हो हल्के मराज् तुम! आओ।’’ मेरे किशोर हठ के सामने परशू बब्बा को मजबूरन मेरी बात माननी पड़ी। वह मशीन के डण्डे पर मेरे दोनों हाथ अपने दोनों हाथों के बीच में रखवाकर कटिया मशीन धीरे-धीरे चलवाते हुए बोले,’’ हां मराज्! एसई मजे-मजे।’’
मैं बहुत जल्दी थक गया। यद्यपि तब बारह-तेरह वर्ष की उम्र में अच्छे स्वास्थ्य की वजह से मैं अपनी वास्तविक उम्र से दो वर्ष बड़ा दिखता था, परन्तु शारीरिक श्रम करने की आदत न होने के कारण मुझे थकान जल्दी आ गयी। मैंने डण्डे पर से अपने हाथ हटा लिये और ज्वार की कटी छोटी-छोटी नरम मीठी गाँठों को छीलकर खाने लगा। ‘‘काए, मराज् थक गए का?’’ “हाँ।” मैंने सिर झुकाए ही कहा।
दुबले-पतले, किन्तु गौर-वर्ण के परशू बब्बा कोई साठ-पैंसठ साल के बूढ़े थे। ढ़लती उम्र में भी इतनी अधिक मेहनत क्यों करते हैं, परशू बब्बा? मैंने जिज्ञासावश उनसे प्रश्न किया,‘‘क्यों परशू बब्बा, आपके घर में कौन-कौन है? आप इतना काम क्यों करते हैं? आपको तो अब आराम करना चाहिए….।’’
‘‘हओ मराज्! अगर काम न करें तो खाएँ का। एक राई-भरी बिन्नूँ है, हमाए …… तुमाए कित्ती हुए या फिन साल खाड़ हल्की हुए।’’ परशू बब्बा के हाथ जल्दी-जल्दी चलने लगे। संभवतः बिन्नूँ की याद आने पर उन्हें घर पहुँचने की जल्दी होने लगी थी। ‘‘बहुत छोटी है, आपकी बेटी।’’ मेरा प्रश्न अपने स्थान पर ठीक था।
‘‘बिन्नूँ हमाई मोड़ी नइयाँ मराज्! नातिन आए वा मोरी।’’ ऊके बाप-मताई हैजा से मर गए ते। तब बा दो महिना की हती। ऊखाँ कछू याद नइयाँ, हमई हाँ अपनो बाप-मताई जानत।’’ परशू बब्बा की आँखें अपने इकलौते बेटे और बहू की याद में सजल हो आईं थीं। ‘‘बिन्नूँ के अलावा अब कोऊ नइयाँ मोरे।’’ खो गये परशू बब्बा दूर कहीं अपने अतीत में।
स्थिति भाँपकर मैंने परशू बब्बा से अगला प्रश्न नहीं किया, जबकि उनसे और बहुत कुछ जानने की इच्छा मेरे मन में जन्म ले चुकी थी। बिन्नूँ से तभी मेरा प्रथम परिचय हुआ था। एक दिन जब मैं अपने स्कूल से वापस आया था, तब मैंने देखा कि हमारे खेतों की देख-रेख करने वाला और पिताजी के आगे-पीछे बंदूक लेकर चलने वाला हाकिम सिंह नीम के पेड़ से बँधे परशू बब्बा को बेशरम की छट्टइया से पीट रहा था। मैं यह दृश्य देखकर अवाक् रह गया। दर्दीली चोटों से परशू बब्बा की कारुणिक चीखें वातावरण में गूँज रही थीं। देखने वाले सहमी आँखों से असहाय परशू बब्बा को दुष्ट हाकिम सिंह के हाथों पिटते देख रहे थे। मैं दौड़कर हाकिम सिंह से भिड़ गया।
‘‘क्यों मार रहे हो परशू बब्बा को?’’ मैं पूरी ताकत के साथ चीखा। हाकिम सिंह का हाथ रुक गया। उसे एकाएक मेरे इस तरह बचाव में आ जाने की उम्मीद नहीं थी। वह बोला,‘‘भैया, ई ने खेतन से जुंड़ी चुराई है। तुम एक कुदई हाँ हो जाओ। मोखाँ ई सारे भड़या की अकल ठिकाने लगाऊन दो।’’ ‘‘जुंडी चुराई?’’ मुझे विश्वास नहीं हुआ। परशू बब्बा चोरी नहीं कर सकते। ‘‘कितनी जुंडी चुराई?’’ ‘‘पसेरक’’
‘‘तुम झूठ बोल रहे हो। परशू बब्बा चोर नहीं हो सकते और फिर थोड़ी सी जुंडी के पीछे क्या तुम इनकी जान ले लोगे, दूर हटो।’’ मैंने हाकिम सिंह के हाथ से बेशरम की उधड़ चुकी छट्टइया छीन ली। परशू बब्बा मार खाकर बेदम हो चुके थे। मैंने उनके शरीर को टटोला, अर्द्ध-नग्न बूढ़े शरीर पर बेशरम की छट्टइया से पड़ चुकी नीली धारियों ने मुझे तुरन्त रोष से भर दिया। अगले ही पल मैंने उसी बेशरम की छट्टइया से दुष्ट हाकिम सिंह के ऊपर वार पर वार करने प्रारम्भ कर दिए।
“तुम जल्लाद हो! तुमने परशू बब्बा पर हाथ उठाया? कितने बूढ़े और कमजोर हैं ये। इन्हें पीटते तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने पिता की उम्र के बूढ़े आदमी को तुमने मारा? तुम राक्षस हो!, तुम जानवर हो! कसाई हो!” रोते-रोते पता नहीं कितनी चोटें मैं हाकिम सिंह पर करता रहा। पता नहीं और क्या-क्या बकता रहा। मैं अपना आपा खो चुका था, एकाएक पैर फिसल जाने के कारण स्वयं सिर के बल गिर कर बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में भी मैं अंट-शंट बकता रहा। मेरे किशोरमन को बेहद ठेस पहुँची थी। उस दिन मेरे पिताजी व माँ घर में नहीं थे। दोनों लोग कहीं गये हुए थे। उन्हें तुरन्त सूचना दी गयी। जब मेरी बेहोशी टूटी, मैंने उन्हें सारी बातें रो-रो कर बतायीं।
पिताजी ने मेरे सामने हाकिम सिंह को बहुत डाँटा और मेरे आग्रह पर परशू बब्बा के इलाज के लिए शहर से डाक्टर को लेकर आने के लिए एक आदमी भेज दिया। डाक्टर साहब के आ जाने पर उनके साथ मैं भी परशू बब्बा को देखने उनके घर गया। गाँव के अन्तिम छोर पर बने कच्चे घरों की पंक्तियों में एक घर परशू बब्बा का था।
परशू बब्बा के घर की कुंडी खटखटायी गई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। दरवाजा एक लड़की ने खोला था ….. मेरी हमउम्र गौर-वर्ण, अति सुन्दर। सौंदर्य जैसे उसके शरीर से फूटा पड़ रहा था। हृष्ट-पुष्ट, गोल-सुडौल उसके हाथ थे। बड़ी-बड़ी हिरणी जैसी आँखें, काली और घनी भौंहे, जैसे ब्रह्माजी ने उसे एकांत में गढ़कर तराशा और संसार में सौंदर्य का एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए भेजा हो। गौर वर्ण, अपूर्व सुन्दर और हिरणी जैसी बड़े नेत्रों वाली लड़की बिन्नूँ थी।
डाक्टर परशू बब्बा को देख रहा था और मैं बिन्नूँ को एकटक निहारे जा रहा था। मेरा किशोर मन यह मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था कि इतनी सुन्दर लड़की परशू बब्बा की नातिन कैसे हो सकती है? वह कितने मैले और गंदे कपड़े पहने रहते हैं । उसे अपने बब्बा के पास जाते घिन नहीं आती होगी। यह स्कूल भी नहीं जाती होगी। मैंने बिन्नूँ से जानना चाहा, “क्यों तुम्हीं बिन्नूँ हो न?’’
“हओ हल्के मराज्! एई आए हमाई राई-भरी बिन्नूँ। बिन्नूँ जेई आए हल्के मराज्, जो तुम्हें पूछत रत।’” परशू बब्बा कराहते हुए बोले। बिन्नूँ ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाते हुए अपनी आँखें भूमि पर गड़ा दीं। परशू बब्बा के घर से वापस आने पर मेरे किशोर मन में खलबली मच गयी। बिन्नूँ की सुन्दर मनोरम छवि मेरी आँखों से एक पल के लिए भी अलग नहीं हो रही थी। उसको पुनः देखने की इच्छा बलवती होती चली गयी।
सच तो यह कि उस दिन से ही मेरे किशोर मन के किसी कोने में बिन्नूँ के प्रति उसकी सुन्दरता और आकर्षण के हवा पानी से दया-मिश्रित प्यार का बीज अंकुरित हो चला था और फिर परशू बब्बा के घर किसी न किसी बहाने पहुँच जाना। बिन्नूँ को अपने घर बुला लेना, साथ-साथ घूमना-फिरना, बैठकर देर तक उससे बातें करने का सिलसिला प्रारम्भ हो गया।
उसका सानिध्य मुझे अच्छा लगता। निश्छल प्रेम हम दोनों के मध्य अपना स्थान बना चुका था। किशोर उम्र होने के कारण हमारे मिलने पर किसी को कोई खास आपत्ति नहीं होती थी। ऊँच-नीच और बड़े-छोटे की सोच वालों को जरुर हम-दोनों का सानिध्य पंसद नहीं आता था।
बिन्नूँ को मैं मन ही मन चाहने लगा था। वह भी मुझे बहुत चाहती थी। मैं जब कभी उसे सताया करता, तो वह रो पड़ती थी। मेरे चुप कराने पर वह भोली बाला बहुत जल्दी चुप हो जाती थी। मैं उसे अपने साथ अक्सर नदी, पहाड़ और जंगल की ओर घुमाने ले जाता। वह मेरी हर बात सहजता से मान जाती थी।
बिन्नूँ को देखे बिना मेरे मन को चैन नहीं पड़ता था। बुन्देली में उसकी बातें मनमोह लेने वाली होती थीं। उसे बहुत बातें करनी आती थीं। वह बहुत तेज और मुझसे अधिक हिम्मती और ताकतवर थी। हँसने से उसके गालों पर गड्ढे पड़ जाते थे। उसकी उन्मुक्त हँसी बहुत प्यारी लगती थी। मुझे सबसे सुन्दर लगती उसकी श्वेत दंत-पंक्ति, जो उसके गुलाबी होठों के खुलते ही चमक उठती थी।
लगभग दो वर्ष हम दोनों का साथ रहा। मैंने इस बीच हाई स्कूल पास कर लिया था। आगे की शिक्षा के लिए मुझे शहर में मामाजी के यहाँ भेजने की तैयारी शुरू होने लगी। बिन्नूँ का बिछोह मेरे लिए असहनीय हो रहा था। मैं तब सोच रहा था कि बिन्नूँ मेरे साथ शहर क्यों नहीं चल सकती? क्या मेरा पढ़ना आवश्यक है? इत्यादि। बिन्नूँ से बिछुड़ने की बात किसी से कह पाना भी मेरे लिए मुश्किल कार्य हो गया था, क्योंकि अब मेरे किशोर मन में समझ ने अपने पैर पसार लिये थे।
……और फिर वह दिन आ गया, जब मुझे गाँव छोड़ना पड़ा। गाँव छोड़ने से कुछ समय पूर्व मैं बिन्नूँ के घर गया। बिन्नूँ ने रो-रोकर अपना बुरा हाल बना रखा था, तब मैंने भावुक हो आवेश में कहा था,”बिन्नूँ! मैं पढ़ लिखकर लौटूँगा और बड़ा होकर तुमसे ही विवाह करूँगा।” भोली बिन्नूँ मेरे द्वारा कहे सीधे-सपाट शब्दों को सुनकर ऐसे मान गयी, जैसे भोले नन्हें बच्चे अपनी माँ के समझाने पर मान जाते हैं और तब अन्तिम बार हम-दोनों बहुत देर तक आलिंगनबद्ध रहे थे। कच्चे अमरूदों का वह चिर-स्मरणीय, सुखद आलिंगन आज भी मेरे स्मृति-पटल पर अच्छी तरह से अंकित है।
मेरे विचारों का क्रम लड़खड़ाया। निद्रा बाधित हुई। बिन्नूँ मेरी पहिएदार कुर्सी के पायताने सिर रखकर सो रही थी, जहाँ पर मेरे दुर्घटना की भेंट चढ़ चुके पैर होने चाहिए थे। नींद में डूबी निश्चित बिन्नूँ के चेहरे पर मैंने दृष्टि जमाई। आज की बिनई काकी के चेहरे पर मैंने वर्षों पहले की बिन्नूँ की छवि ढूँढ़ने की बहुत कोशिश की, पर वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। हम सभी समय के फेर में हैं।
मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और बिन्नूँ गाँव-भर की बूढ़ी बिनई काकी बन चुकी है। गाँव में बनी हमारी पुश्तैनी हवेली, उसके फर्नीचर सब थोड़े-बहुत परिवर्तन के साथ यथावत हैं। बदलाव आया है, तो हम दोनों में। इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आते-जाते रहेंगे। कहानियाँ बनती-बिगड़ती रहेंगी। सदा के लिए हम जैसे जीवित लोग नहीं रहेंगे, जबकि जड़, निर्जीव व प्राकृत वस्तुएँ थोड़े-बहुत परिवर्तन के साथ सदैव बनी रहेंगी।
समय अपनी गति से आगे खिसकता रहा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, गाँव के कुछ लोग मेरे विरोधी होते चले गए। लोगों ने तरह-तरह की काल्पनिक कथाएं गढ़नी शुरू कर दीं थीं। व्यंग्य और परिहास के छीटें जब-तब मेरे व बिन्नूँ के आसपास आकर गिरने लगे थे, परन्तु वह आज भी अटल, अविचलित मेरी सेवा में निःस्वार्थ भाव से समर्पित बनी हुई है। उसने मुझे कभी यह आभास भी नहीं होने दिया कि मैं अपाहिज हूँ। इस जीवन में बिन्नूँ सामाजिक दृष्टिकोण से मेरी जीवन-संगिनी तो नहीं बन सकी, किन्तु वह मेरे शरीर के अंगों के रूप में मेरे हाथ, पैर, आँखें बन चुकी थी। …. और अधिक कहूँ, तो वास्तव में अब वह मेरी सब कुछ बन चुकी है।
बुन्देली झलक (बुन्देलखण्ड की लोक कला, संस्कृति और साहित्य)
लेखक-महेन्द्र भीष्म