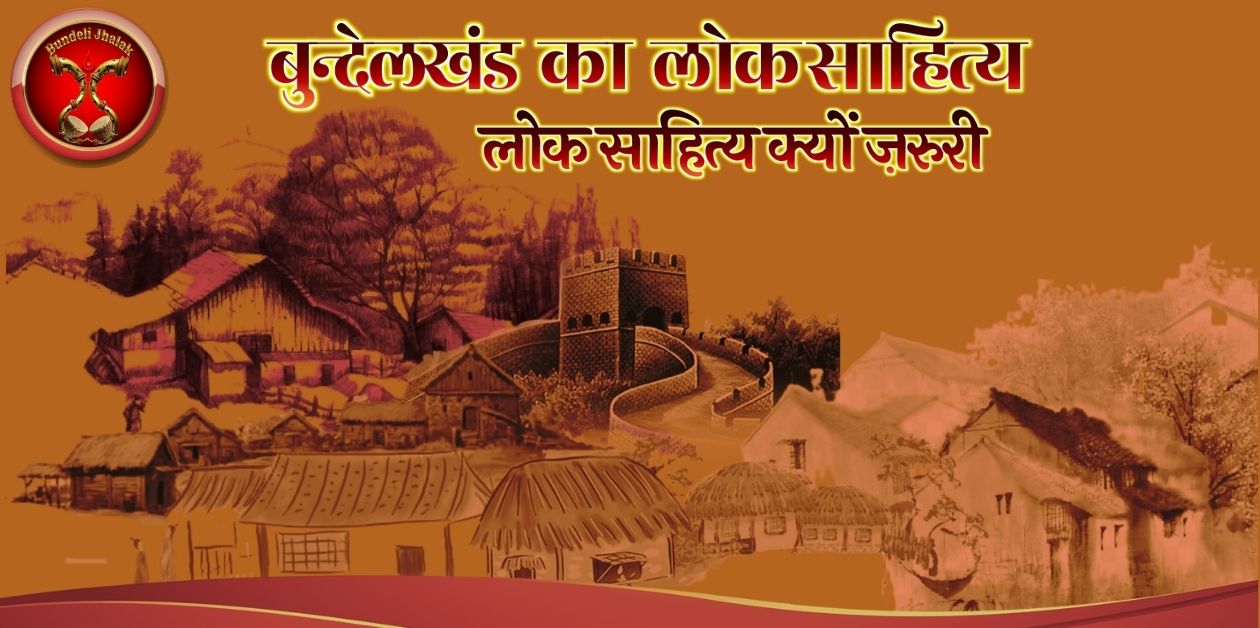किसी भी समाज मे Loksahitya Kyon Zaruri है ? इसकी क्या प्रासांगिकता है? बदलाव के हमलों से गुजरना हर समाज की नियति है। कभी वह परम्परा की शक्ति बटोरकर उनसे टकराती है, संघर्ष करती है और जय-पराजय के द्वन्द्व में जूझती कोई एक किनारे आ खड़ी होती है, लेकिन कभी वह रूढ़ियों की कमजोरियों के कारण बदलाव को सफेद झंडी देकर सन्धि कर लेती है, कट्टरपंथियों से बार-बार लड़ती है और बदलते मूल्य को अपनी परम्परा में शामिल कर अपना बना लेती है।
समाज निर्माण मे लोकसाहित्य की भूमिका
समाज की यह सन्धि और जूझ उसकी गतिशीलता की पहचान है और गति का क्रमिक प्रवाह उसका इतिहास। संघर्ष और समझौते की शक्ति और सहनशीलता, बदलते मूल्यों की उपयोगिता एवं गति-अगति के रेखाचित्रा की परख समाज की समझ और जागरूकता का परिणाम है।
बदलाव की प्रकृति, उसका आयाम और समाज की प्रकृति से उसका मेल जानना जितना जरूरी है, उतना ही उसके परिणामों पर विचार करना। कहीं ऐसा न हो कि कोई प्रगति का नुस्खा छूट जाय और हम पचास वर्ष पिछड़ जाएँ अथवा कोई घातक प्रहार हमारी समाज की मूल प्रकृति को ही बदल दे और दुनिया के सामने हमारी पहचान ही लुप्त हो जाए।
समाज का आत्म-निरीक्षण एक अनिवार्य कर्म है, खासतौर से इस शती के इस अन्तिम दशक में, जबकि बदलाव के घात-प्रतिघात परम्परा की देह को निरन्तर प्रताड़ित कर रहे हैं। आजादी के बाद देश का विकास जरूरी था और उस विकास के लिए कोई सोची-समझी नीति और कार्य की दिशा तै करनी थी, जिसके लिए देश की जनता से संवाद और सम्पर्क से प्राप्त अनुभवों की पूँजी अर्जित करना चाहिए था।
गाँधीजी ने जिस भारतीय समाज को बहुत करीब से परखकर हर काम की भागीदारी के लिए सक्रिय बनाया था, उसे शासक वर्ग ने उपेक्षित रखा और रईस देशों की तकनीकी विकास के अनुकरण में संलग्न हो गए।
परिणाम यह हुआ कि समाज में एक तरफ पूँजीवादी वर्ग पैदा हुआ, जिससे भौतिकता की होड़ बढ़ी और जीवन में यान्त्रिकता आती गई; दूसरी तरफ बेरोजगारी का शिकार वर्ग अपराधिक कार्यों से जुड़ गया तथा तीसरी तरफ उत्पादक और उपभोक्ता के बीच एक दलाल वर्ग बना, जिसने शोषण के नायाब तरीके निकाले। चोरी-डकैती और अपहरण, नकली उत्पादन और कला व्यापार तथा गैरकानूनी धन्धों और दंगों की निरन्तर बृढ़त का कारण भौतिक मानसिकता और जबरन लादी हुई बेकारी है।
आर्थिक विकास से जुड़ी भौतिक मानसिकता के साथ आई आधुनिकता की प्रवृत्ति जिसने सबसे पहले धनिकों पर अपना मन्त्रा फूँका और बाद में मध्यम वर्ग पर, खासतौर से मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों पर। आधुनिकता की मेनका ने अच्छे-अच्छे विश्वामित्रों को हिला दिया। खूब चर्चा हुई उसकी लेकिन आधुनिकता के नाम पर पश्चिमीकरण का बोलबाला रहा। पश्चिम की भोगोन्मुखी जीवनपद्धति और पश्चिम की विचार प्रणालियाँ। दोनों ने इस देश की देह और मन को काफी प्रभावित किया, पर आत्मा को छू तक नहीं पाए।
ललित कलाओं पर पश्चिमी प्रभाव से प्रकट है कि एक हद तक मन भी पश्चिमी विचार धाराओं से संवेदित हो उठा था, लेकिन पश्चिम का भोगवाद तो उस दौर में काफी समय तक छाया रहा और आज भी उसकी पैठ कम नहीं है। पश्चिमीकरण के अदृश्य बीजों से इस उपजाऊ धरती पर मानसिक दासता, धार्मिक कट्टरता, जातिवाद, साम्प्रदायिकता आदि के कई अंकुर फूटे और उनकी पौध लहलहा उठी। पौधालय बन गए और पौध मुफ्त बँटने लगी। सबसे बड़ा खतरा है मानसिक दासता से, जो बौद्धिक प्रतिबद्धता के स्कूल खोलती है और बौद्धिक उपनिवेशवाद के पाठ सिखाती है।
धार्मिक कट्टरता पहले अपने धर्म की रक्षा के लिए पनपी थी, आज भी उसका उद्देश्य वही है, लेकिन लाभों के दायरे चौड़े हो चुके हैं। साम्प्रदायिकता धर्मिक कट्टरता की ही सहेली है, पर है बहुत चंचल और मनचली। इसीलिए लोग जल्दी रीझ जाते हैं और उसके इशारों पर आशिकों की तरह नाचते रहते हैं। जातीयता (जातिवाद) बूढ़ी खाला हैं, उनका अच्छा नाम लोगों ने छीन लिया और तंग कोठरी में बैठा दिया, लेकिन राजनीतिक गणिका अब उसमें मन्त्रा सीखने आने लगी है, जिससे खाला का महत्त्व बढ़ गया है और वह अब इतराकर नए-नए मंचों पर बैठे अपने पक्ष में संगठन करने लगी है।
विदेशी ऋण बार-बार हरकारे की तरह देश का दरवाजा खटखटाता है और साहूकारों के रुक्कों पर लिखी शर्तों के नीचे दस्तखत करवा लेता है। या तो कच्चा माल सस्ते मूल्य पर लेने की या अपना तैयार माल गलाने की। उदारीकरण की उदारता तो जगप्रसिद्ध है। हमने कब किसको रोका ? पुर्तगीज और डच आए, फ्रांसीसी आए और अंग्रेज आए। हमने खुले मन से उनका स्वागत किया, आज भी कर रहे हैं। विदेशी कम्पनियाँ व्यापार करेंगी, माल यहीं तैयार कर बेचेंगी। उनकी पूँजी, तैयार माल और उनका क्रय-विक्रय देखकर हमारी देशी कम्पनियों का स्तर ऊँचा उठेगा।
कोई हर्ज नहीं कि हमार कच्चा माल सस्ते में जाए और उनके तैयार माल का ‘बाजार’ बन जाए। हमारी सरकार सबकुछ के लिए तो है ही, आखिर देश तो हमारा है। ‘मार्केट’ भले ही उनका हो, पर है तो हमारे देश में। फिर हमारी कम्पनियाँ भाड़ झोंकती रहेंगी ? होड़ है, पर कहाँ नहीं है होड़। विदेशों में भी होड़ है। इस देश को भी होड़ का सामना करना ही पड़ेगा। अपने देश में होड़ करने लगें, तो विदेश में भी कर सकेंगे। फिर जाएँगे कहाँ, हमारे देश के नियम-कानून मानना ही पड़ेगा।
व्यापार के बढ़ाव से अर्थ की महिमा बढ़ेगी, पर आदमी बौना होता जाएगा। आदमी मशीन की तरह चलेगा, मशीन की तरह पैदा करेगा और मशीन की तरह जिएगा। संवेदनहीन और आदमियत के सभी रिश्तों और गुणों से दूर, केवल आदमियत का मुखौटा लगाए।
अब तो मशीन का साम्राज्य है और फैल गई है उसकी सेना। बाहर से आया है इलेक्ट्रोनिक मीडिया का कप्तान, जो अपने कम्प्यूटरों की फौज से आदमी के हिसाब-किताब, अभिलेख-आँकड़े आदि ही नहीं, आदमी की कविता, संगीत, चित्राकला आदि तक कैद करवा रहा है।
परिणाम यह होगा कि लेखाकार, कलाकार आदमी हट जाएगा और मशीन ही छा जाएगी। मशीन ही गायेगी, मशीन ही चित्र बनाएगी और मशीन ही कविता पढ़ेगी। आदमी का आदमी से संवाद खत्म। संवादहीनता-दर-संवादहीनता। शहरी गुरू के चेले बनने लगे हैं हमारे गाँव। राजनीति, गुटबन्दी, जातिवाद की चालें चलनेवाले खिलाड़ी बैठे रहते हैं शहरों में, हुक्म देते हैं गाँवों के मुखियों, पंचों, सरपंचों को और तब चलते हैं मुहरे बने गाँव के लोग।
शतरंज की बाजियों में आतंक, गुंडागर्दी, कलह, आरोप-प्रत्यारोप, झगड़े-फसाद, और कूटनीति की सभी शहमातें शुरू हो गईं। सादगी, भोलापन, नैतिकता आदि चरित्र के सभी गुणों की मात होने लगी। कथावार्ता के अलाव बन्द हो गए, पनघट का पनरस चला आया और ग्रामीण उद्योग एवं कला-कौशल डूबने की कगार पर हैं। सबसे बड़ी बात है भीतर से आत्मीयता, मेल-जोल, प्रेम और रस के भाव रीत गए, बाहर से मिठबोले, जालसाजी और दिखावे के नाटक शुरू हो गए !
आदमी पूरा-का-पूरा व्यस्त। औरतें व्यस्तता की दौड़ में आगे बढ़ने को आतुर। पति-पत्नी, पिता-पुत्रा और बहिन-भाई में संवाद नहीं। सिनेमा और दूरदर्शन की भोगोन्मुखी संस्कृति हावी। त्यौहारों, पर्वों और उत्सवों पर लोकगायकों की जगह कैसिटों के फूहड़ और बेमले गीत। जीवन को देखने तक के लिए समय नहीं, जीवन से साक्षात्कार समाप्त। गाँव-नगर और देश के कल्याण के सोच की तरफ किसका ध्यान है ? देश की पहचान और राष्ट्रीय अस्मिता की प्रतीक भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए कौन तैयार है ? सीस उतारै भुइँ धरै जो चलै हमारे साथ…।
‘जो आबै सन्तोष धन, सब धर धूरि समान’
‘हुई है वही जो राम रचि राखा’
‘कोऊ नृप होइ हमें का हानी, चेरी छाँड़ि न होइब रानी’,
मुखिया मुखसों चाहिए, खान-पान को एक।
पालै-पोसै सकल अंग, तुलसी सहित विवेक।।’,
‘जे गरीब पर हित करें, ते रहीम बड़ लोग’,
‘टूटे सुजन मनाइये, जो टूटें सौ बार’,
‘रहिमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून।
पानी गये न ऊबरें, मोती मानस चून।।’
‘जिस कुल देश जाति के बच्चे, दे सकते हैं निज बलिदान।
उसका वर्तमान कुछ भी हो, पर भविष्य है महा महान।।’ और न जाने कितने तरह के विचार, लेकिन सवाल है सबको मिलाकर सोचने का…
‘हम कौन थे क्या हो गए, और क्या होंगे अभी ?
आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएँ सभी।’
सोचना दिमाग का काम है, पर संवेदन हृदय का। हृदय में लोक से जुड़ने का स्वभाव है, इसीलिए तो वह किसी की पीड़ा से तुरन्त द्रवित हो जता है। पीड़ा चाहे वह व्यक्ति की हो, चाहे गाँव या देश की। दिमाग उसे भले ही रोके, पर वह उसका भी कहना टाल देता है। आज की संवेदन और संवादहीनता का एक ही इलाज हैµहृदय, हृदय का लोक से जुड़कर लोकहृदय होना। लोकहृदय चेतना का वह सागर है, जो पूरे विश्व को तरंगायित करने की अपार क्षमता रखता है। सवाल है लोकहृदय की चेतना जगाने का और उत्तर है…
हृदय को उद्वेलित करनेवाले लोकसाहित्य का फैलाव। लोकसाहित्य एक ऐसा कीमती रत्न है, जो छोटे-बड़े, गोरे-काले, अमीर-गरीब सभी के पास रहता है और सभी के उपयोग का है। उसका स्वामी न तो कोई एक वर्ग है, न एक जाति और न एक सम्प्रदाय। वह न तो पूँजीपति की तिजोरी में कैद किया जा सकता है और न जमीन के नीचे किसी अजगर की हिरासत में रखा जा सकता है। वह तो लोकधन है, जो लोक के लिए लोकमुख में रहता है।
लोक यानी कि शिक्षित-अशिक्षित, धनी-निर्धन, मजदूर-मालिक, कृषक-व्यापारी, ग्रामीण-नागरिक सभी लोक हैं। केवल गाँवों के गँवारों को लोक कहना उचित नहीं। लोक साहित्य सभी का है। पितृधन पिता से पुत्र या पुत्र को मिलता है और पुत्र जब पिता बनता है, तब वह उसमें कुछ और जोड़ या घटाकर अपनी सन्तान को देता है। इसी तरह लोकसाहित्य का लोकधन एक युग के लोक से दूसरे युग के लोक को मिलता है, और लोक अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे ग्रहण करता है।
हर युग में नए सृजन को लोक द्वारा लोक की कसौटी पर कसकर अपनाया जाता है और वही लोकसाहित्य में शामिल हो पाता है। आज जरूरत है ऐसे ही लोकसाहित्य की, जो आदमी में आत्मीयता, सहानुभूति, प्यार, उत्साह और रस पैदा कर सके तथा जो आर्थिक भेद-भाव, मशीनी जकड़न और तमाम द्वेषों के खिलाफ जूझ सके।
रह गई राष्ट्रीय अस्मिता की सुरक्षा की समस्या, तो उसके लिए देश की लोकसंस्कृति का प्रसार ही सुनिश्चित हल है। लोकसंस्कृति लोक की संस्कृति है, किसी खास वर्ग, जाति या सम्प्रदाय की नहीं। उसके लोकदर्शन में किसी खास दर्शन या मतवाद और लोकधर्म में धार्मिक कट्टरता एवं साम्प्रदायिकता के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।
उसका घटक मनुष्य केवल मनुष्य होता है, जो मनुष्यत्व की संपूर्ति में लगा रहता है। कुंठा, निराशा, अनास्था जैसी वैयक्तिक मनोदशा से लेकर परिवार की कलह, टूटन जैसी सामूहिक परिणति तक जिन मानसिक तनावों को आज का व्यक्ति भोग रहा है, उनका उपचार लोकसंस्कृति की आशा, आस्था, आत्मीयता आदि से संपुष्ट निश्छल दृष्टि करती है। मशीनी यान्त्रिकता और विज्ञानी बौद्धिकता के लगातार हमलों से निरन्तर बचाने का काम लोकसंस्कृति ही करती रही है।
लोकसंस्कृति ही भारतीय संस्कृति की जड़ है। उसी के रस से भारतीय संस्कृति का पौधा पल्लवित, पुष्पित और सुफलित है। उसी की कर्माश्रथी ऊर्जा से वह संघर्ष करती है और विजातीय तत्त्वों से रक्षा करती है। कितनी विदेशी संस्कृतियाँ आईं और कितने आक्रामक दबाव डाले गए, लेकिन लोकसंस्कृति ने अपने लोकाचरणों से उन्हें दूर हटा दिया।
उसकी जुझारू शक्ति चुपचाप अपना काम करती है। जरूरत है लोकसंस्कृति को और अधिक अपनाने की, ताकि राष्ट्रीय स्मिता बनी रहे और दुनिया के सभी देशों में उसकी आभा दमकती रहे। ऐसी लोकसंस्कृति को प्रकाश में लाने का माध्यम है लोकसाहित्य, वह लोकसाहित्य, जो संघर्शधर्मी ऊर्जा से परिपूर्ण है।