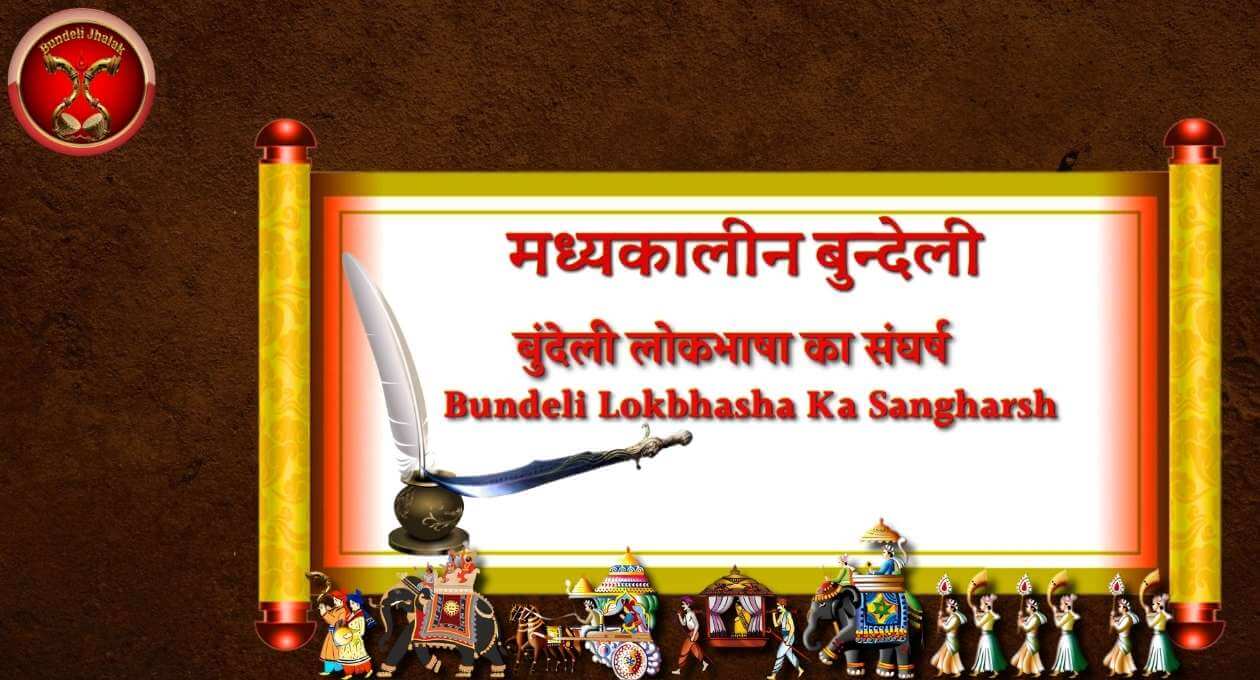बुन्देलखंड मे मध्यकालीन काल मे विदेशी आक्रमणो और उनके शाशनकाल मे आयतित तुर्की, फारसी और अरबी भाषाओं के प्रभाव से उनके प्रचार-प्रसार से संगीत तथा भाषा पर कब्जा जमा लिया था जिससे Bundeli Lokbhasha Ka Sangharsh काफी बढ गया था ।
बुंदेली लोकभाषा के ऐतिहासिक दस्तावेज
बुन्देलखंड लोकभाषा का उदय नवीं शती में हो चुका था। विशेषतया बुन्देली का, क्योंकि ग्यारहवीं शती के प्रारम्भ में ही चन्देल नरेश गंडदेव का लोकभाषा में कविता रचने का प्रमाण मिलता है। निजामुद्दीन कृत तकबात-ए-अकबरी से पता चलता है कि उसने 1023 ई. में महमूद गजनवी से सन्धि के समय एक कविता भेंट की थी, जो लुगत-ए-हिन्दुई या हिन्दवी में थी।
कुछ इतिहासकारों ने इस घटना को असिद्ध ठहराया है। पर उन्हे इस तथ्य से कोई आपत्ति नहीं होगी कि उस समय लोकभाषा में कविता लिखी जाने लगी थी। इस घटना (चाहे वह अपने पक्ष में गढ़ी गई हो) में लोकभाषा की इस स्थिति का सत्य छिपा हुआ है और उससे साबित होता है, कि उसके दो सौ वर्ष पहले लोकभाषा का जन्म हुआ था। बारहवीं शती में तो लोकभाषा का उत्कर्ष जगनिक के आल्हखंड लोकमहाकाव्य में दिखाई पड़ता है, जिसकी रचना 1182 और 1193 ई. के बीच किसी समय हुई थी।
दूसरे जनपदों में भी लोकभाषा के विकास के ऐसे साक्ष्य खोजे जा सकते हैं। भाषा के बढ़ाव की इस स्थिति में एक तूफानी आँधी की तरह हिन्दवी या हिन्दुई आयी और देश के उत्तर तथा दक्षिण में एक साथ फैली। राजाश्रय पाकर उसकी सीमाएँ इतनी बढ़ीं कि देश के कोने-कोने तक उसका असर हुआ। सूफी अनुयाइयों के दल-के-दल अपने धर्म के प्रसार-प्रचार के लिए देश के भीतरी गाँवों तक अपने फड़ जमाते थे और उस समय के संगीत तथा भाषा पर कब्जा जमा लेते थे।
इस गम्भीरता परिस्थिति ने लोकभाषा को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया था और भाषाकारों के लिए चिन्ता खड़ी कर दी थी। फल यह हुआ कि लोकभाषा संघर्ष के लिए बाध्य हुई, लेकिन आश्चर्य तो यह है कि उसके इस तीन सौ वर्षों के लम्बे संघर्ष को किसी भी इतिहासकार ने नहीं पहचाना और उसे सिर्फ किसी भी इतिहास ग्रन्थ में स्थान नहीं मिला।
वस्तुतः इस ऐतिहासिक संघर्ष को समझने के लिए उस समय की उन सभी परिस्थितियों को गहराई से देखने की जरूरत है, जिन्होंने भाषा को नागफाँस की तरह जकड़ लिया था। बारहवीं शती के अन्तिम दशक में दिल्ली-अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद मुस्लिम शासन की स्थापना हुई और सोलहवीं शती के प्रथम चरण तक गुलाम, खिल्जी, तुगलक, सैय्यद और लोदी वंशों ने राज्य किया।
उनके बाद दक्षिण में गोलकुंडा और बीजापुर तथा उत्तर में मुगल साम्राज्य ने विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार जमाया। इस कारण तेरहवीं शती से शासन की कामकाजी और दरबार की भाषा तुर्की, फारसी से लदी रही। आप कहने को उसे हिन्दवी कह लें, किन्तु अमीर खुसरो ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है ‘‘प्रत्येक सौ कोस पर भारतीय बोलियाँ बदल जाती हैं, किन्तु लगभग चार हजार फर्लांग के क्षेत्र में फारसी भाषा वही है। इतनी महान भाषा हमारी बोलचाल का माध्यम है।
दिल्ली शासन के समक्ष फारसी को शासकीय भाषा के रूप में प्रयोग करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था।’’ प्रकट है कि फारसी को बहुत सोच-समझकर राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था और इसका सीधा प्रभाव जनता के उस वर्ग पर अधिक पड़ा, जो राजसेवा में था या राजाश्रय का इच्छुक था। फिर शासकों की भाषा या राजभाषा का दबदबा इतना होता है कि शासित जनता या आम आदमी का उसकी प्रभाव परिधि से छूटना कठिन होता है।
इतिहासकारों ने तो यह भी जानकारी दी है कि लूट के माल में भी सूफियों का हिस्सा रहता था। जगह-जगह खानकाहों (सूफी मठों) का निर्माण बादशाहों ने ही करवाया था। मतलब यह है कि मुसलमान बादशाहों ने हर तरह से सूफियों को बढ़ावा दिया था और वे भी बादशाहत का पूरा ध्यान रखते थे। सूफियों के अचरजभरे चमत्कारों, सभी के प्रति समान प्रेम भावना और उपेक्षित एवं दलित वर्ग के प्रति उदारता से साधारण जनता और खासतौर से अछूत एवं पिछड़े वर्ग के लोग इतने अधिक सम्मोहित हुए।
शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने 1186 से 1235 ई. तक एक करोड़ हिन्दुओं को सूफी बनाकर एक मिसाल ही खड़ी कर दी। अपने धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए उन्होंने लोकभाषा अपनाई, उसी में उपदेश दिए और धार्मिक गीत रचे। साथ ही कव्वालों की एक ऐसी सेना पैदा कर दी, जिसके दल-के-दल हर जगह अपने करतब दिखाने में बेजोड़ साबित हुए।
उन्होंने हिन्दवी के रूप में एक नई भाषा खड़ी कर दी, जो लोकभाषा के स्थान पर प्रतिष्ठित होने का दावा करने लगी। जनता में भी भारतीय मुसलमानों का एक ऐसा वर्ग खड़ा हो गया, जो हिन्दू माताओं और विदेशी पिताओं के संस्कार, धर्म और भाषा का असमान मिश्रण था। इस वर्ग की भाषा फारसी शब्दों से बोझिल हिन्दवी थी। इस प्रकार सूफियों ने एक तरफ धर्म और संस्कृति तथा दूसरी तरफ संगीत और भाषा में बदलाव लाने का प्रयास किया था। यह कहना कठिन है कि दो-तीन सौ वर्षों तक निरन्तर जारी रहने वाला उनका यह उपक्रम पूर्व नियोजित था या स्वतः फूटने वाला एक सहज परिणाम।
तीसरा पक्ष है मुसलमान और मुगल बादशाहों के आश्रित काजियों और मौलवियों का जो अपने धर्म और भाषा के कट्टर समर्थक थे। वे शासन-व्यवस्था के अनिवार्य अंग थे और उनके बिना नीति का निर्धारण होना मुश्किल था। यहाँ तक कि कुछ अहम् मसलों पर बादशाह तक को झुकना पड़ता था। उनके प्रभाव के अनेक उदाहरण इतिहास में मिलते हैं और कहीं-कहीं बादशाहों की हठीली बान के भी।
इतना तो सत्य है कि दरबारों में तुर्की, फारसी और अरबी भाषा के कवियों और विद्वानों तथा विदेशी पद्धति के कलाकारों को ऊँचा दर्जा प्राप्त था। उनके ओहदे और सम्मान को देखकर भारतीय कवियों, विद्वानों और कलाकारों ने भी अपने-आप परिवर्तन कर लिया था। सभी कलाओं में विदेशी असर फैलने लगा था और भाषा पर भी उसका दबाव स्वाभाविक था। इन परिस्थितियों ने लोकभाषा की बाढ़ को तो रोका ही, एक गम्भीर समस्या भी खड़ी कर दी और वह है हिन्दवी या हिन्दुई का नया भाषा-रूप।
दक्षिण में तुरूबक भाषा और उत्तर में दक्खिनी हिन्दी नामों से प्रचलित इस भाषा रूप में नए पद, कव्वालियाँ, गजलें आदि लिखे गए और उनके फड़ों ने लोकभाषा का स्थान लेना शुरू कर दिया। इस भाषा में विदेशी शब्दों की ही भरमार थी, केवल एक-दो शब्द लोकभाषा से लिए जाते थे और उनका रूप भी बदला हुआ होता था। नमूने के लिए शेख फरीदुद्दीन गजशंकर (तेरहवीं शती का पूर्वार्द्ध) की दो पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत हैं।
पाक रख तूँ दिल को गैर सेती आज साई फरीद का आवता है।
कदीम कदीमी के आँवने से लाजवाल दौलत को पावता है ।।
इनमें आवता, आँवने, पावता जैसे शब्दरूपों पर ध्यान दें, तो उनमें भी एक बदलाव दिखाई देता है, शेष तो फारसी अरबी के हैं। कुछ बहुत थोड़े से इने-गिने कवियों को छोड़कर सभी ने ऐसे ही भाषा रूप को अपनाया है, जिसे लोकभाषा कहना उचित नहीं है। इसके अलावा खास बात है भाषा के रुख या प्रवृत्ति की और इस दृष्टि से हिन्दवी ने लोकभाषा के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था।
हिन्दवी का लक्ष्य सूफी मत का प्रचार था, भाषा का प्रसार नहीं। इसलिए प्रचारात्मकता के तौर पर उसे लोकभाषा कहा गया। तीसरे, दरबारी गद्य तो पूरा-का-पूरा विदेशी था, जिसके प्रभाव का नमूना आज भी कचहरी-अदालत के गद्य में मिलता है। अगर लोकभाषा संषर्घ न करती, तो उसका हाल कचहरी के गद्य जैसा होता। इस स्थिति के बावजूद संगीत के एक प्रतिष्ठित विद्वान ने हिन्दवी को लोकभाषा मान लिया है।
विष्णुदास ग्वालियर के तोमर नरेश डूँगरेन्द्रसिंह (1424-55 ई.) के समकालीन थे। उनके समय जैनकाव्य की भाषा अपभ्रंशमिश्रित थी, जो जनसाधारण की भाषा से हटकर थी। अपभ्रंश मिश्रित भाषा रूप में संस्कृत के शब्दों को भी गृहीत किया गया था, परन्तु वह लोक को प्रभावित करने में समर्थ नहीं था। तीसरा नाथपन्थी भाषारूप था, जिसमें संस्कृत का बहिष्कार किया गया था। चौथा हेमचन्द्र का ग्राम्य अपभ्रंश का था, जो प्राचीन गुजराती का पर्याय था।
मतलब यह है कि इन भाषारूपों में लोकसहजता का अभाव था और वे विशिष्ट वर्गों तक ही सीमित हो गए थे। समकालीन कवि विद्यापति की पदावली का प्रभाव पूर्व की ओर ही रहा और कबीर की भाषा न तो मुस्लिम भक्तों को मान्य हुई, न हिन्दू भक्तों को। सूफियों ने तुर्की, फारसी, अरबी आदि विदेशी भाषाओं का सहारा लिया था, तो विष्णुदास ने संस्कृत को अपनाकर लोकभाषा को ऐसा रूप दिया, जो सर्वमान्य हो सके।
कव्वाली के जवाब में उन्होंने विष्णुपद रचे, जिनसे अष्टछाप की वीणाएँ बजीं और सूर तथा तुलसी जैसे महाकवियों ने अमूल परिवर्तन ही उपस्थित कर दिया। मध्य प्रदेश की गेय पद-परम्परा तो काफी पुरानी थी, पर विष्णुदास के भक्ति-परक विष्णुपद चुनौती के रूप में रचे गए थे। महाभारत (1435 ई.) और रामायण (1442 ई.) की रचना भी इसीलिए हुई थी, कि प्रबन्धकाव्य की धारा को एक नया मोड़ दिया जा सके।
राजा ने ऐसी काव्य रचना के लिए विष्णुदास को तंमोर (पान का बीड़ा) दिया था और कवि ने बीड़ा उठाकर उस चुनौती को स्वीकारा था। उसने ऐसे काव्य को भाषा काव्य बनाई ही कहा था, और यह लोकभाषा की अगुवाई का पुष्प नक्षत्र था, क्योंकि विष्णुदास की परम्परा बैजू, बख्शू आदि गायकों से होकर सूर, तुलसी आदि कवियों के द्वारा पूरे देश में छा गई थी और हिन्दवी का वह भाषा रूप धीरे-धीरे गायब हो गया था।
कुछ विद्वान और संगीतज्ञ विष्णुपदों की निर्मित और नामकरण में ग्वालियर के तोमर नरेश मानसिंह (1486-1519 ई.) को श्रेय देते हैं, पर यह उचित नहीं है। इतना अवश्य है कि मानसिंह ने अपने राज्यकाल में विष्णुपदों की समृद्धि और उनके प्रसार में अपना महत्त्वपूर्ण योग दिया था, लेकिन पद-परम्परा को नया जीवन और गाथा को नया रूप देने का प्रवर्तक कार्य विष्णुदास का था।
संघर्ष का दूसरा अखाड़ा था संगीत। सूफियों की दृष्टि से खुदा के ध्यान में गाना- बजाना और नाचना इस्लाम धर्म के अनुसार वैध ही नहीं, आवश्यक भी है। यह बात अलग है कि काजी और मौलवी उसे त्याज्य ही मानते रहे, परन्तु सूफियों के बादशाहों पर प्रभाव और राजनीति में संगीत के दखल के कारण उनकी एक न चली।
निश्चित है कि उत्तर भारत के भारतीय संगीत में कोई उत्साह नहीं रह गया था और विदेशी संगीत धीरे-धीरे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा रहा था। खुसरो ने भारतीय रागों की व्यवस्था मुकाम पद्धति से की थी। उनके इन्द्रप्रस्थ मत या मेल सिद्धान्त को, जो कि मुकाम पद्धति का ही नया नाम था, पूरे देश में फैलाने का काम सूफी गायकों ने किया। तेरहवीं से पन्द्रहवीं शती तक भारतीय संगीत का कोई ग्रन्थ नहीं रचा गया। इस शून्य से भारतीय संगीत की अपार क्षति तो हुई ही, लोकभाषा को भी संगीत के माध्यम से जो फैलाव मिलता, उससे वंचित रहना पड़ा।
बुन्देली झलक (बुन्देलखण्ड की लोक कला, संस्कृति और साहित्य)
संदर्भ-
बुंदेली लोक साहित्य परंपरा और इतिहास – डॉ. नर्मदा प्रसाद गुप्त
बुंदेली लोक संस्कृति और साहित्य – डॉ. नर्मदा प्रसाद गुप्त
बुन्देलखंड की संस्कृति और साहित्य – श्री राम चरण हयारण “मित्र”
बुन्देलखंड दर्शन – मोतीलाल त्रिपाठी “अशांत”
बुंदेली लोक काव्य – डॉ. बलभद्र तिवारी
बुंदेली काव्य परंपरा – डॉ. बलभद्र तिवारी
बुन्देली का भाषाशास्त्रीय अध्ययन -रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल