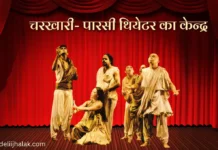नौटंकी हाथरस शैली और कानपुर शैली दो मशहूर शैली से निकली बुन्देलखण्ड मे स्वांग के मिश्रण से स्थापित Bundelkhand Ke Nautankibaz का अलग ही विधान है। एक जमाना था जब खासकर गाँवों,कस्बों और शहरों में किसी के विवाह,जन्म दिवस समारोहों, मेलों आदि उत्सवों में मनोरंजन के लिए लोकनाट्य “नौटंकी” कंपनी का आना बड़ा ही शान का विषय माना जाता था। लोगबाग चार – चार कोस दूर से चलकर नौटंकी का आनंद लेने आते थे।रात-रात भर नक्काड़े के मीठे बोल गूँजा करते थे –
क्डाधिं, धिडनग, क्डां, धिनक, किड़नग, घ्ड़ां, धाड़धा, क्डधा, नड़, तड़ा, …
उन दिनों मनोरंजन के कोई खास साधन नहीं थे।रामलीला, स्वांग, लोकनाट्य नौटंकी ही गाँवों वालों के लिए जानकारी प्रदान कराने, सामाजिक कुरीतियों से परिचित कराने का एक सस्ता किंतु स्वस्थ मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञानवर्धन के भी सहज सुलभ साधन माने जाते थे।
जहाँ तक नौटंकी का संदर्भ है तो वास्तव में नौटंकी एक प्रसिद्ध लोकनाट्य है जिसमें रसीले संवादों और गीत – संगीत की प्रधानता तो होती ही है, इसमें पद्यात्मक संवादों के साथ -साथ कथानक में वीर तथा शृंगार रस पर भी खासकर जोर दिया जाता है।
नौटंकी ‘स्वाँग‘ और ‘लीला‘ के समान ही लोकनाट्य का प्रमुख रूप है। इसका प्रारम्भ मुग़ल काल से पहले का है। रासलीला के समान ही इसका रंगमंच भी अस्थिर, कामचलाऊ और निजी होता है। लोकनाट्य नौटंकी अत्यंत ही लोकप्रिय और प्रभावशाली लोकनाट्य कला रही है।
भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में जिस सट्टक को नाटक का एक भेद माना है, इसके विषय में जयशंकर प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि सट्टक नौटंकी के ढंग के ही एक तमाशे का नाम है।
इतिहासकार बताते हैं कि नौटंकी में यों तो कोई भी प्रसिद्ध लोककथा खेली जा सकती है किंतु श्रृंगार रस प्रधान अथवा प्रेमगाथा की कोटि की रचनाएँ ही प्रधानता पाती रही हैं। प्रेमलीला अथवा रोमांच का संस्पर्श किसी न किसी रूप में होना ही चाहिए। इसी को नौटंकी भी कहा जाता है। नौटंकी मूलत: किसी प्रेम कहानी केवल “नौ टंक तौलवाली ” कोमलांगी नायिका होगी। वही संगीत-रूपक में प्रस्तुत की गयी और वह रूप ऐसा प्रचलित हुआ कि अब प्रत्येक संगीत-रूपक या स्वाँग ही नौटंकी कहा जाने लगा है।
हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार नौटंकी का वर्तमान रूप चाहे जितना आधुनिक हो, उसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं। रामबाबू सक्सेना ने अपनी पुस्तक ‘तारीख़-ए-अदब-ए-उर्दू‘ में लिखा है कि ‘नौटंकी लोकगीतों और उर्दू कविता के मिश्रण से पनपी है।’वहीं कालिका प्रसाद दीक्षित कुसुमाकर का मानना है कि ‘नौटंकी का जन्म संभवतः ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी में हुआ था।’ 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो के प्रयत्न से नौटंकी को आगे बढ़ने का अवसर मिला। खुसरो ने अपनी रचनाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया है, वैसी ही भाषा और उन्हीं के छंदों से मिलते-जुलते छंदों का प्रयोग नौटंकी में बढ़ने लगा।
उत्तर प्रदेश,पंजाब, राजस्थान आदि में सुल्ताना डाकू, भक्त पूरनमल, सत्यवादी हरिश्चंद्र, लाला हरदौल, रावण – अंगद संवाद , आल्हा आदि लोकगाथाओं का मंचन प्रमुख रूप से किया जाता था। प्राचीनकाल में तो इस नौटंकी में पुरुषों द्वारा ही स्त्रियों पात्रों के अभिनय किये जाते थे।
कालांतर में नौटंकी में तवायफों का प्रवेश शुरू हो गया। एक जमाने तक कानपुर की मशहूर अदाकारा रसूलन बाई की मौजूदगी नौटंकी के मंचों पर पाकीजगी की पर्याय बनी रही। समय के साथ नौटंकी के मंचों पर सस्ती लोकप्रियता भुनाने के चक्कर में तबायफों के भड़काऊ नृत्यों को तरजीह मिलनी शुरू हुई जो अश्लीलता परोसने में भी परहेज नहीं करती थी। इसीके साथ नौटंकी जैसे स्वस्थ मनोरंजन करानेवाले इस लोकनाट्य की उल्टी गिनती शुरू हो गई…।
आज यह लोकनाट्य नौटंकी लगभग समाप्त होने की कगार पर हाँफती हुई खड़ी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी बड़े शहरों लखनऊ,आगरा, मेरठ, वाराणसी, गाज़ीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, बलिया, मथुरा आदि में दर्जनों नौटंकी और थियेटर कम्पनियाँ थीं। आज ये नौटंकी कंपनियाँ और थिएटर प्रायः अब मृतप्राय हैं।
मैंने सन 1990 के दशक में अपने सुरीलों के गाँव क्योलारी, जालौन, उरई, कोंच, झाँसी, कानपुर, बाँदा आदि स्थानों के नौटंकी से जुड़े तमाम कलाकारों से संपर्क करते हुए उनकी समस्याओं को विभिन्न माध्यमों से उठाया था। उस समय नौटंकी कला केन्द्र के बाँदा के निदेशक श्री शंकर स्वरूप सक्सेना, जालौन के पण्डित पूरन महाराज,सहाब (जालौन) के छदामी लाल मास्टर , ढोलक वादक पण्डित रामगोपाल तिवारी लौना (कोंच) के रामप्रकाश महाराज , कोंच के भाँड़ परंपरा के उस्ताद गफूर खान, उरई के मम्मू मास्टर।
मलकपुरा के सत्तार खान, बंगरा के लालजी साहब, सुढार सालावाद के बद्रीशरण मिश्रा के अलावा क्योलारी के कीर्तिशेष पूजनीय पिताश्री गंगादीन मास्टर, उस्ताद मेंहदी हसन साहब, आदरणीय ग्याप्रसाद कुशवाहा जी, कीर्तिशेष बड़े भाई सरयू प्रसाद भारती जी, हरफनमौला कलाकार आदरणीय रामबिहारी पाँचाल, हमारे बाबा आदरणीय हल्केराम नेताजी, श्री सियाशरण बुधौलिया, शेखपुर बुजुर्ग के नक्काड़ची चाचा परमाई मास्टर।
जालौन के हीरालाल जौकर, कुठौंद के मिश्रीलाल नृत्यकार,सिमरिया गाँव के सुरेश डांसर, कुदरा कुदारी के गोविंद मस्ताना, झाँसी के नाथूराम साहू कक्का,झाँसी में ही नक्कारों के मुहल्ला के मंसूर,ललितपुर की चंदाबाई बेड़नी, कानपुर मूलगंज की नृत्यांगना शबनम,महोबा के पंचम सहित नौटंकी क्षेत्र के बहुतेरे कलाकारों से प्रत्यक्ष मिला एवं उनके साक्षात्कार किए थे।
आज भी मैं कलाजगत के नये पुराने चेहरों से समय-समय पर मिलता रहता हूँ। जब 1990 के दौरान मैं जनपद जालौन ही मेरा कार्यक्षेत्र और केन्द्र था तब उसी दौरान कला,संगीत और साहित्य के संवर्द्धन के लिए समर्पित अखिल भारतीय स्तर पर काम करने वाली एक राष्ट्रीय संस्था के उस समय के तथाकथित लोककला प्रमुख से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मेरे द्वारा संकलित एवं लिखित यह संपूर्ण जानकारी यह कहकर मुझसे लेली थी, कि वे उसे प्रकाशित कराएंगे … ……।
मगर अफसोस, मैंने दो सालों में जिन पारंपरिक लोकगीतों, लोकसंगीत , लोकनाट्यों,आदि से संबंधित विविध सामग्री गाँव – गाँव जाकर संकलित की थी, उसी सामग्री को उन स्वयंभू लेखक महोदय ने थोड़ा- बहुत रद्दोबदल करके अपने नाम से, अपने पद और रुतबे का बेजा इस्तेमाल करते हुए खुशी -खुशी प्रकाशित कराली।
शायद इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हमारे पुरखों ने कहा होगा –
तेल जरै बाती जरै , नाम दीया का होय।”
खैर ! मसिजीवियों के साथ इस तरह के हादसे होते ही रहते हैं…. हम सभी लोगों ने आपस की नाटकीय बातचीत के दौरान अक्सर सुना होगा ये “नौटंकी बंद करो”आज सच्चे अर्थों में वह नौटंकी बंद ही हो गई है। नौटंकी कंपनियों से जुड़े हुए हजारों – हजार कलाकार भुखमरी के शिकार हैं। नौटंकी जैसी लोकनाट्य कला पूरी तरह से दमतोड़ रही है। नौटंकी के साथ ही नौटंकी के छंद भी बेदम नजर आ रहे हैं। नौटंकी में प्रयोग किए जाने वाले चौबोला,लावनी, दौड़ और बहरतवील जैसे छंद अब पुरानी किताबी तिजोरियों तथा तहखानों के काले अँधेरों में कैद हैं।
फिर भी मैं “बहरतवील” जैसी अत्यंत लोकप्रिय नौटंकी मशहूर गायन शैली (छंद विधा) को काली अँधेरी सुरंग से निकालकर आपके सम्मुख इस आशय से उपस्थित कर रहा हूँ,कि कभी जगमग रही नौटंकी और उसकी बेहरतवील को कुछ रोशनी मिल सके –
बहरतवील
मोटेतौर पर ‘बहरतवील‘ शब्द का अर्थ लंबी कविता होता है।यों तो ‘बहर‘ उर्दू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ सामान्यतः छंद ही होता है। बहर का प्रयोग गजल लेखन में विशेष तौर पर किया जाता है। छंद में लिखी जाने वाली हर लेखन की विधाओं के कुछ अपने – अपने नियम होते हैं।
बहर एक ऐसा माध्यम है जिसमें निश्चित मात्राओं से कड़ियाँ बनीं रहती है ताकि एक ही लय और भार में उसके समान पँक्तियाँ लिखीं जा सकें। मुगल काल के समय नौटंकी के संवादों व गायन शैली में अधिकतर उर्दू ,फारसी मिश्रित हिन्दी शब्दावली का प्रयोग किया जाता था। जिसके प्रभाव से “बहरतवील” जैसी गायन शैली नौटंकी में प्रयोग में आई।
श्रीकृष्ण द्वारा रचित नौटंकी ‘लंकाकांड’ में अंगद-रावण संवाद की एक बेहतरीन बहरतवील का उदाहरण में यहाँ रख रहा हूँ जिसमें अँगद रावण को समझते हुए कह रहा है-
बहरतवील
जादूगर भी बदन भर के टुकड़े करे,
वीर लेकिन जगत में कहाता नहीं।
अपने मुँ करता अपनी बड़ाई है तू ,
शर्म खाता नहीं – शर्म खाता नहीं।
सदगती चाहता है जो लंकापति ,
तो वचन क्यों मेरे ध्यान लाता नहीं।
देके तूँ राम को माँ जनक नंदिनी
यश कमल जगत में खिलाता नहीं।।
जैसे ही बहरतवील का आखिरी शब्द आता वैसे ही नक्काड़ची “रैला” बजाते हुए दौड़ लगाना शुरू कर देता। रंगभूमि में एक ओर गायकों, वाद्य वादकों का समूह भी रहता था , जो अभिनय, संवाद, नृत्य की तीव्रता, उत्कटता को बढ़ाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान रहता था। ढोलक, तबला और नगाड़े का विशेष प्रयोग होता था। ढोलक, तबले के तालों और नगाड़े की चोबों की गूँज रात में मीलों सुनाई पड़ती थी। पैरदान वाले हरमोनियम की मीड़ें ,सारंगी की दर्द भरी सीना चीरने वालीं गमकों के आकर्षण से सोते हुए ग्रामीण भी नौटंकी देखने पहुँच जाते थे…..।