बुन्देलखण्ड में लोकचेतना, लोकभाषा और लोकसाहित्य का उद्भव 9वीं शती में हुआ है। 9वीं शती में अनेक जन-जातियों (गौंड, कोल, भील आदि) थी उनका मनोरंजन कथा-वार्ता, लोकनृत्य एवं लोकनाट्य आदि थे। बुन्देलखंड का लोक नाट्य स्वाँग जिसे Bundelkhand ka Swang कहते हैं। यह भक्तिपरक, हास्यपरक, व्यंग्य-विनोद परक, जातिपरक होते हैं। इन्हे लघु नाटिका भी कह सकते हैं।

Bundelkhand ka Swang के उद्भव का प्रश्न कठिन है, 8वीं-9वीं शती के लोकचेतना के उत्थान-काल में शुरू हो गया था। 9वीं शती मे लोकचेतना का बिस्तार हुआ और लोकगाथाओं, लोकनृत्यों एवं Bundelkhand ka Swang लोकनाट्यों का उद्भव हुआ। 10वीं शती के खजुराहो के मंदिरों में उत्कीर्ण लोक-संगीत और लोकनृत्यों के दृश्य, 11वीं शती के प्रबोध चन्द्रोदय की रंगस्थली महोबा के मदन सागर के बीच पड़े रंगशाला के अवशिष्ट और 12वीं शती के लोकगाथात्मक महाकाव्य आल्हखण्ड से यह निर्णय लेना कठिन नहीं है कि बुन्देलखण्ड में लोकचेतना, लोकभाषा और लोकसाहित्य का उद्भव 9वीं शती में हुआ है तथा 12वीं शती तक उसका चरम उत्कर्ष रहा है।
बुंदेली स्वाँग के उद्भव और विकास का भी यही समय उचित ठहरता है। मध्यकाल में अनेक ग्रंथों में स्वाँग के उल्लेखों से स्वाँग के द्वितीय उत्थान का पता चलता है। आधुनिक युग में स्वाँग पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इतना निश्चित है कि स्वाँग में ही आधुनिक समाज-चेतना, उसकी अनुभूतियों और व्यंजनापुष्ट अभिव्यक्तियों को अपने में समेट लेने की पूरी क्षमता है। बुंदेली स्वाँगों का वर्गीकरण कई दृष्टियों से किया जा सकता है।
1- पौराणिक स्वाँग या धार्मिक स्वाँग जैसे दूध को स्वाँग, माखन-चोरी कौ स्वाँग, राधका कनैया के झगड़े कौ स्वाँग।
2- सामाजिक स्वाँग जैसे जातिपरक स्वाँग, ब्याव के स्वाँग, समस्यापरक स्वाँग आदि।
3- त्यौहार और उत्सवों के संस्कृतिपरक स्वाँग जैसे होरी के स्वाँग, पथरियाऊ चैथ कौ स्वाँग आदि।
4- व्यक्तिपरक रंजन के लिये काल्पनिक स्वाँग जैसे बिच्छू कौ स्वाँग, जेठ दाऊजू, भोरी फुआ, छबीली जिजी, मँझली कक्को, चटकारी भौजी आदि के परिहासपरक स्वाँग।
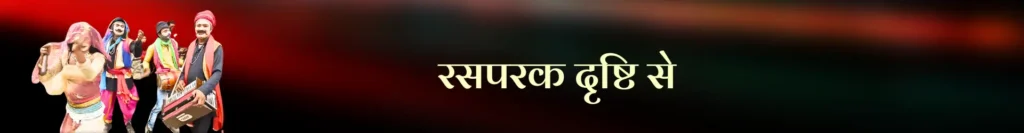
1- श्रृंगारिक स्वाँग जैसे ब्याव के स्वाँग।
2- भक्तिपरक स्वाँग जैसे दूध कौ स्वाँग, माखन चोरी कौ स्वाँग आदि।
3- हास्यपरक स्वाँग जैसे होरी के स्वाँग।
4- व्यंग्य-विनोद परक स्वाँग जैसे दहेज कौ स्वाँग, बिच्छू कौ स्वाँग, जेठ दाऊजू, भौरी फुआ आदि के स्वाँग।
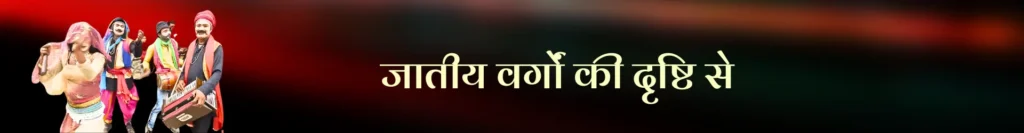
1- धोबी के स्वाँग।
2- कोरी कौ स्वाँग।
3- ब्राह्मनन कौ नकली ब्याव कौ स्वाँग ।
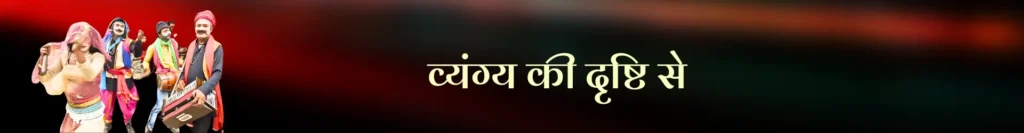
1- हास्यपरक स्वाँग, जैसे-होरी के स्वाँग।
2- उपहासपरक स्वाँग जैसे दहेज कौ स्वाँग।
3- विरोधमूलक व्यंग्य प्रधान स्वाँग, जैसे जेठ दाऊ जू, मंझली कक्को, छबीजी जिजी के स्वाँग।
4- कटूक्तिपरक स्वाँग, जैसे चलौनयाऊ को स्वाँग।
5- विनोदपरक स्वाँग, जैसे बिच्छू कौ स्वाँग।
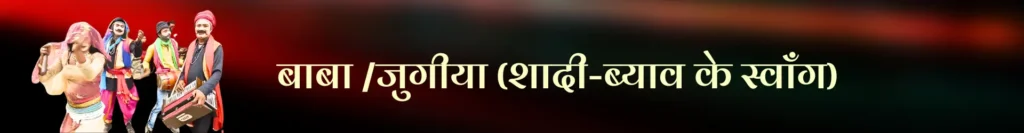
बुंदेलखंड प्रदेश में सबसे अधिक प्रसिद्ध ब्याव के स्वाँग हैं, जो अधिकतर वर पक्ष के घर में बारात जाने पर स्त्रियों के द्वारा अभिनीत किये जाते हैं। कहीं-कहीं इन्हें बाबा-बाई के स्वाँग कहा जाता है। स्त्रियाँ बाबा के प्रदर्शन मे किसी सीमा तक कुछ भी कह सकती हैं या गालियाँ दे सकती है, मज़ाक में मार भी सकतीं हैं । अश्लील तत्व का पुट होने से इन स्वाँगों में पुरुषों और बालकों को अनुमति नहीं दी जाती है।
स्त्रियाँ स्वाँग के अनुरूप सहज उपलब्ध वेश-भूषा धारण करती हैं, किन्तु वह भी अपने में एक वैशिष्ट्य रखती हैं। साड़ी साफा का और घाँघरा धोती का रूप ले लेती है। स्त्रियाँ ही पुरुष पात्र बनती हैं और मरदानेपन की नकल उनके बीच हास्य का कारण होती है। पात्रों का अभिनय कालशून्य होते हुए भी अपना अलग कलात्मक महत्व रखता है। संवाद गद्य और पद्य दोनों में होते हैं। उनकी भाषा सहज बुन्देली होती है, यद्यपि कभी-कभी खड़ी बोली का खड़ापन उसमें घुलमिल जाता है।
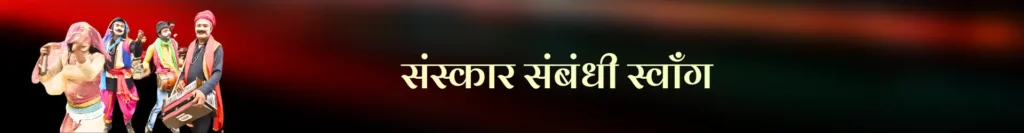
सगनौती कौ स्वाँग, जिसमें एक स्त्री चादर डाल कर उल्टी लेट जाती है और सगनौती को उठाने पर बिन बोले संकेत करती है। राजस्थानी ‘‘टूँटिया-टूँटकी’’ से मिलता-जुलता नकली ब्याव कौ स्वाँग है, जो ब्राह्मणों में प्रचलित है और जिसमें वर-वधू के अभिनय में टीकादि, विवाह के नेगादि सम्पन्न किये जाते हैं।
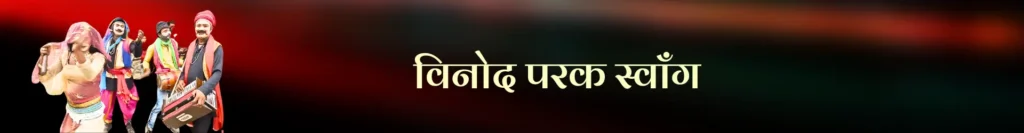
राजस्थानी ‘‘बेरी‘‘ की तरह माँई जू को स्वाँग , जिसमें एक स्त्री चादर ओढ़कर माँई जू बनती है और ऊँचा सुनने या बहरी होने के कारण अटपटा उत्तर देती है। इसी तरह बिच्छू कौ स्वाँग में एक स्त्री एक गीत गाती हुई बिच्छू के काटे की भावुक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करती है और लोकप्रचलित है कि अभिनय की प्रस्तुति में बिच्छु चढ़ जाता है।
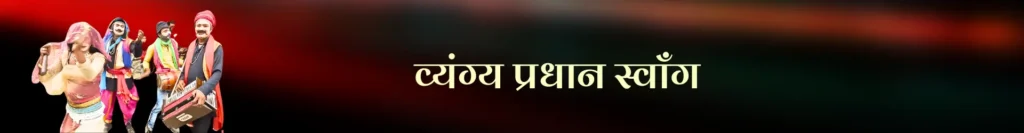
जैसे दहेज कौ स्वाँग , जो उपहासपरक होता है और चलौनयाऊ कौ स्वाँग , जो कटूक्तिपरक होने के कारण सीधी चोट करता है।
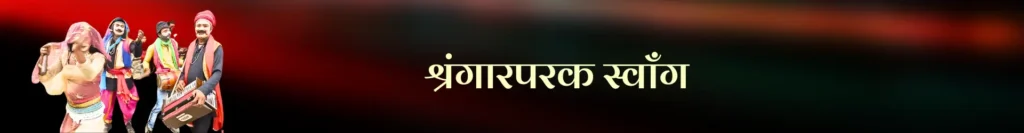 जिन्हें बाबा के स्वाँग कहते हैं और जिनमें दाम्पत्य जीवन के सम्भोग तक का चित्रण रहता है। अश्लील गालियाँ तक दी जाती हैं। मर्यादा और संयम से दूर ये स्वाँग आलोचना के शिकार हुए हैं, किन्तु यह ध्यान में रखना जरूरी है कि वे कामेच्छा के मार्गीकरण में उपकरण रूप में उपयोगी भी हैं।
जिन्हें बाबा के स्वाँग कहते हैं और जिनमें दाम्पत्य जीवन के सम्भोग तक का चित्रण रहता है। अश्लील गालियाँ तक दी जाती हैं। मर्यादा और संयम से दूर ये स्वाँग आलोचना के शिकार हुए हैं, किन्तु यह ध्यान में रखना जरूरी है कि वे कामेच्छा के मार्गीकरण में उपकरण रूप में उपयोगी भी हैं।
 जैसे दध कौ स्वाँग और माखन चोरी कौ स्वाँग, जिनमें कृष्ण की लीलाओं को आंचलिक रूप दिया गया है।
जैसे दध कौ स्वाँग और माखन चोरी कौ स्वाँग, जिनमें कृष्ण की लीलाओं को आंचलिक रूप दिया गया है।
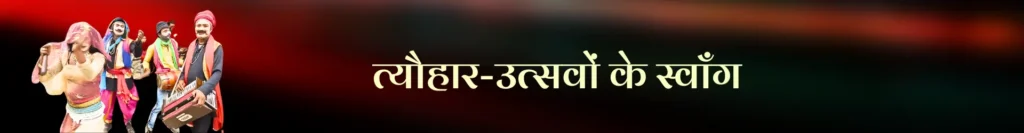
होली, जलविहार, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, राम-विवाहोत्सव आदि में नाना प्रकार के स्वाँगों का प्रचलन रहा है और आज भी जीवित है। होली में गधा की सवारी, उल्टी खाट, राधाकिसन की फाग, परिया टूटने कौ स्वाँग आदि हास्य-विनोद की दृष्टि से होते हैं। जलविहार में विमानों के जुलूस, शिवरात्रि में शिव की बारात और रामविवाह में राम की बारात के साथ तरह-तरह के स्वाँगों की प्रथा बहुत पुरानी है।
स्वाँगों की एक विशेषता यह है कि इनमें तत्कालीन संदर्भों के साथ बदलाव भी आता गया है और इस तरह उनकी गतिशील प्रवृत्ति बराबर बनी रही है। जन्माष्टमी में धँदकानौ कौ स्वाँग बहुत प्रसिद्ध है। बालकों द्वारा अभिनीत यह स्वाँग कृष्ण की दध लीला को साकार करता है।
इसी प्रकार बालकों द्वारा कृष्ण-जन्म की बधाई घर-घर देने और दही-पँजीरी लेने का आग्रह करने का स्वाँग- ‘‘बधाई कौ स्वाँग’’ खेला जाता है, जो आज भी हर जाति के बालकों का प्रमुख आकर्षण बना हुआ है।
कार्तिक स्नान (कातिक-अन्हाबौ) में कतकारीं कृष्णलीला से संबंधित कुछ स्वाँग रचती हैं, जिनमें कतकारीं छैंकबे कौ स्वाँग, जो दानलीला के आधार पर बना है और राधा-कृष्ण के झगड़े कौ स्वाँग, जो मानलीला से संबंधित है।
इन स्वाँगों में सबसे अलग, किन्तु बहुत महत्वपूर्ण स्वाँग ‘‘कजरियाँ छैंकबे कौ स्वाँग’’ है, जो सावन की पूर्णिमा या परमा को होता है। महोबा में कजरियों का बहुत बड़ा मेला लगता है। जब कीरतसागर की तरफ कजरियों का जुलूस चलता है, तब आल्हा की बैठक के नीचे पहली सीढ़ी पर कजरियाँ छेंकी (रोकी) जाती हैं।
यह स्वाँग और सजीव हो उठता है, जब पुरुष पात्र ही चन्द्रावलि, आल्हा, ऊदल, लाखन, पृथ्वीराज चैहान के वेश में अभिनय करते हैं। चन्द्रावलि दोनों हाथों में कजरियों के दौने लिए हुए बैलगाड़ी में बने डोले पर चलती है।
आल्हा, ऊदल, लाखन, पृथ्वीराज चैहान के वेश में अभिनय करते हैं। आल्हा, ऊदल और लाखन जोगी के वेश में और पृथ्वीराज हाथी पर सवार होकर तालाब तक जाता है। वहाँ पृथ्वीराज के हार कर भागने के बाद चन्द्रावलि कजरियाँ खौंटती है और झूला झूलती है।
इस अवसर पर सावन गीतों का सामूहिक गान स्वाँग को और भी प्रभावी बना देता हैं यह स्वाँग चन्देलों और चैहानों के बीच कजरियों के युद्ध का चित्र उपस्थित करता है, जिसमें जोगी बने आल्हा-ऊदल ने अपने शौर्य से पृथ्वीराज चैहान को खदेड़ कर अपनी बहिन चन्द्रावलि (चँदेल नरेश परमर्दिदेव या लोकविख्यात परमाल की पुत्री) की कजरियाँ खुटवायीं थीं।

इस अंचल की विभिन्न जातियाँ-भंगी, धोबी, कोरी, कुर्मी, चमार, काछी, बारी आदि द्वारा विविध स्वाँग विवाह एवं अन्य अवसरों पर आनन्दोल्लास के साथ अभिनीत किये जाते हैं। उनमें पुरुष पात्रों की बहुलता रहती है, पर स्त्री पात्र भी कम नहीं रहते। हँसी-ठिठोली से भरे संलाप और मुक्त नृत्यों का आवर्तन आकर्षक प्रभाव छोड़ते हैं। ढोलक, मंजीरा, खँजड़ी, कसावरी आदि लोकवाद्यों के साथ गीतों और कभी-कभी नृत्यों का सम्मिलन स्वाँगों में सरसता ला देता है। बीच-बीच में बुंदेली गद्य की हास्यपरक पंक्तियाँ दर्शकों को आह्लादित करती हैं।
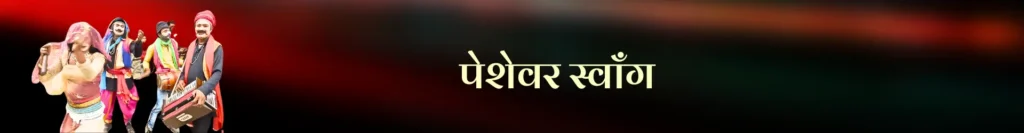
मध्ययुग में स्वाँग-मण्डलियों का उदभव हुआ था। रियासतों के समय तक ये घूम-घूम कर स्वाँगों का प्रदर्शन करती रही हैं। बहुरूपियों के स्वाँग तो अब भी गाहे-बगाहे देखे जाते हैं। भाँड़ों की भँड़ैती रियासती-काल तक प्रसिद्ध रही है। वेश्याओं (पतुरियों) के स्वाँग उनके गीत और नृत्य के साथ प्रचलित रहे हैं। बहुधा उत्सवों, शादियों और जुलूसों में पेशेवर स्वाँग होते रहे हैं।
संवाद छोटे, सरल और सरस होते हैं। उनकी भाषा सहज सीधी-सादी होती है, जिसे आम आदमी समझ सकता है। बुंदेली का अकृत्रिम और चलताऊ रूप गद्य और पद्य दोनों में दिखाई पड़ता है।
कृष्ण: हमाई राधा प्यारी चंदा सी उजयारी, सूरज कैसी जोत, मोतिन कैसी पोत कनैर कैसी डार, लफ-लफ दूनर हो जाय, सोरा सिंगार करें, बारा आभूसन पैनें, फूलन सें तुलनवारी, नैनू कैसौ लौंदा……………..तुमनें कऊँ देखी
(राधा-किशन को स्वाँग)
गीत:
दइरा मोरो लै लो बिहारी नँदलाल, दइरा मोरो लैलो।
कोरी कोरी मटकी में दइरा जमाओ, पानी न डारो इक बूँद।
दइरा.कौना सहर की तू है गूजरी का है तुमारौ नाँव।
मथुरा सहर की हम हैं गूजरी राधा हमारो नाँव।
कितने सेरै तुमरो दइरा बिकानो का है तुमरो मोल।
टकै सेर मोरौ दइरा बिकानो लाख टका है मोल।
(दध को स्वाँग से)
इसमे गीत के साथ राधा और कृष्ण नृत्य भी करते हैं। बुंदेली स्वाँगों में नृत्य, गीत और अभिनय की त्रिवेणी बहती है, वास्तव में बुंदेली स्वाँग अभिनय प्रधान हैं, गीत और नृत्य बीच-बीच में गुँथे रहते हैं। कुछ स्वाँग अवश्य गीतनृत्यपरक हैं, जैसे बिच्छू कौ स्वाँग में सिर्फ एक लम्बा गीत है और अभिनेत्री अकेले गीत गाती है तथा उसकी पंक्तियों के अनुरूप अभिनयात्मक नृत्य करती है।
बिच्छू चढ़ जाने पर उस भाव की पूरी अभिव्यक्ति नृत्य के माध्यम से होती है। नृत्य की त्वराएँ पीड़ा की तीव्रता का बोध कराती हैं। वैसे स्वाँगों में अभिनय की परिपक्वता नहीं होती और न उसके लिये कोई तालीम या अभ्यास का प्रयत्न किया जाता है। आंगिक और वाचिक अभिनय ही प्रमुखतः प्रयुक्त होता है, आहार्य पर कम ध्यान रहता है और सात्विक के लिए कोई स्थान नहीं।
वस्तुतः अभिनय की सहजता ही उनकी विशेषता है। संकेतों द्वारा अभिनय से और भी सहजता आ जाती है। बुंदेली स्वाँगों में अभिनय, गीत और नृत्य का ऐसा मेल दिखाई पड़ता है, जो उन्हें विशुद्ध स्वाँगों के रूप में प्रतिष्ठित करा देता है। वे नाटक पहले हैं, गीत, संगीत और नृत्य बाद में।
रूपयोजना और रंगमंच की दृष्टि से बुंदेली स्वाँग और भी सहज है। ब्याव के स्वाँगों में रंगमंच घर का आंगन होता है, उसी में फर्श, दरी, चादर आदि बिछा दी जाती है। पेशेवर और लोकोत्सव के स्वाँगों में खुला मंच, ऊँचा चबूतरा, ऊँची जमीन या तख्त होता है।
परदों का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था जरूरी होती है। काँड़रा और रावला तो जमीदार के दरवाजे या गाँव के किसी भी घर के सामने खुले मैदान में खेला जाता है। रूप-सज्जा सीधी-सादी और आसानी से प्राप्त प्रसाधनों से युक्त होती है। स्वाँग के उपयुक्त वेशभूषा धारण करना आवश्यक है।
राधाकिसन को स्वाँग में कृष्ण के लिये पीला वस्त्र या उत्तरीय, साड़ी की धोती और काछनी, मोरपंख और मुरली काफी है। काँड़रा में सराई के ऊपर घाँघरा जैसा चुन्नटदार झामा और पगड़ी मुख्य अभिनेता की पोशाक है। मुख-सज्जा कोयला, काजल, खड़िया, मुर्दाशंख, रज आदि देशी प्रसाधनों से करते हैं, लेकिन कृष्ण-राधा को सफेद-पीले चंदन और श्री से सजाते हैं। इस तरह मंच और सज्जा के फेर से स्वाँग प्रायः मुक्त रहता है।
हर प्रकार के स्वाँग में अलग-अलग लोकवाद्यों का प्रयोग होता आया है, जिसका अनुसरण बहुत थोड़े परिवर्तन के साथ आज तक चला आ रहा है। ब्याव के स्वाँगों में ढोलक, मंजीरा, झाँझ और झौंका, लेकिन रावला में सारंगी और मृदंग की जगह हारमोनियम और ढोलक भी आ गये हैं। पेशेवर स्वाँगिये तो और भी स्वतंत्र हैं, उन्होंने हारमोनियम जैसे नये वाद्यों को अपना लिया है।
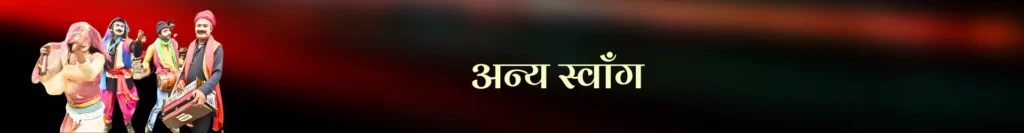 अन्य स्वाँग मे जैसे ताना-बाना कौ स्वाँग, चुरेरिन कौ स्वाँग, कुँजरा-कुँजरिया कौ स्वाँग आदि। राजस्थानी ‘‘ताणा’’ की तरह ‘‘ताना-बाना कौ स्वाँग’’ में ताना-बाना बुनने के रूप में स्त्री-पुरुष के मेल से सुखद दाम्पत्य की अप्रत्यक्ष सीख मिलती है। चुरेरिन कौ स्वाँग में चूड़ियों के महत्व का संकेत है और कुँजरा-कुँजरिया कौ स्वाँग में उनकी झगड़ालू प्रवृत्ति की झांकी है। इन स्वाँगों में मनोरंजन के साथ नारी जीवन के कुछ पहलुओं पर सीख का बंधन-सा प्रतीत होता है, किन्तु वह उजागर न होकर यथार्थ के परदे से ढका रहता है।
अन्य स्वाँग मे जैसे ताना-बाना कौ स्वाँग, चुरेरिन कौ स्वाँग, कुँजरा-कुँजरिया कौ स्वाँग आदि। राजस्थानी ‘‘ताणा’’ की तरह ‘‘ताना-बाना कौ स्वाँग’’ में ताना-बाना बुनने के रूप में स्त्री-पुरुष के मेल से सुखद दाम्पत्य की अप्रत्यक्ष सीख मिलती है। चुरेरिन कौ स्वाँग में चूड़ियों के महत्व का संकेत है और कुँजरा-कुँजरिया कौ स्वाँग में उनकी झगड़ालू प्रवृत्ति की झांकी है। इन स्वाँगों में मनोरंजन के साथ नारी जीवन के कुछ पहलुओं पर सीख का बंधन-सा प्रतीत होता है, किन्तु वह उजागर न होकर यथार्थ के परदे से ढका रहता है।
संदर्भ-
बुंदेली लोक साहित्य परंपरा और इतिहास – डॉ. नर्मदा प्रसाद गुप्त
बुंदेली लोक संस्कृति और साहित्य – डॉ. नर्मदा प्रसाद गुप्त
बुन्देलखंड की संस्कृति और साहित्य – श्री राम चरण हयारण “मित्र”
बुन्देलखंड दर्शन – मोतीलाल त्रिपाठी “अशांत”
बुंदेली लोक काव्य – डॉ. बलभद्र तिवारी
बुंदेली काव्य परंपरा – डॉ. बलभद्र तिवारी
बुन्देली का भाषाशास्त्रीय अध्ययन -रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल




